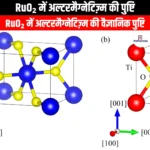13 new amphibian species discovered in Northeast India

संदर्भ:
हाल ही में वाइल्डलाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ़ इंडिया (WII), देहरादून द्वारा पूर्वोत्तर भारत में 13 नई उभयचर (Amphibian) प्रजातियों की खोज की घोषणा की गई है। यह खोज भारत में पिछले दशक में एक ही शोध प्रकाशन में वर्णित कशेरुकी प्रजातियों की सबसे बड़ी संख्या है।
पूर्वोत्तर भारत: जैव-विविधता का वैश्विक हॉटस्पॉट
पूर्वोत्तर भारत—विशेष रूप से अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, असम, नागालैंड—इंडो-बर्मा जैव-विविधता हॉटस्पॉट का हिस्सा है। इस क्षेत्र की कठिन भू-आकृति, उच्च वर्षा, घने वनों और अलग-अलग ऊँचाई वाले क्षेत्रों ने अत्यंत विशिष्ट प्रजातियों को जन्म दिया है। यही वजह है कि इस क्षेत्र में छिपी हुई प्रजातियों (Hidden Biodiversity) का पता लगाने के लिए आधुनिक टैक्सोनोमिक तरीकों की आवश्यकता रही है।
नई खोज की प्रमुख विशेषताएँ:
- WII द्वारा घोषित 13 नई प्रजातियाँ मुख्यतः बश फ्रॉग्स (Bush Frogs) की श्रेणी से संबंधित हैं। पहले भारत में 82 बश फ्रॉग प्रजातियों का विवरण उपलब्ध था, जिनमें से 15 पूर्वोत्तर में पाई जाती थीं। इस नई खोज ने इस संख्या को उल्लेखनीय रूप से बढ़ा दिया है।
- सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि: 13 में से 6 प्रजातियाँ अरुणाचल प्रदेश से मिलीं, 3 मेघालय, 1-1 प्रजाति असम, मिजोरम, नागालैंड और मणिपुर से मिली तथा 7 प्रजातियाँ संरक्षित क्षेत्रों (Protected Areas) से खोजी गईं।
- अरुणाचल प्रदेश में सबसे अधिक 6 प्रजातियों की खोज हुई, जिनमें— नमदाफा टाइगर रिज़र्व से 2 प्रजातियाँ, ईगलनेस्ट वाइल्डलाइफ सेंक्चुरी से 1 प्रजाति, मेहाओ वाइल्डलाइफ सेंक्चुरी से 1 प्रजाति शामिल हैं।
- यह अध्ययन ध्वनिक विश्लेषण (Acoustics), आनुवंशिक अध्ययन (Genetics), और आकृतिक अध्ययन (Morphology) को समन्वित करके किया गया। इसमें 81 स्थलों, जिनमें 25 संरक्षित क्षेत्र शामिल हैं, से सैंपल एकत्र किए गए। अध्ययन में पुराने संग्रहालय संग्रह (Museum Collections) की पुनः समीक्षा की गई।
उभयचर प्रजाति क्या हैं?
- उभयचर वे कशेरुकी जीव (vertebrates) हैं जो जल और थल दोनों में जीवन व्यतीत करते हैं। इनका नाम Amphibia इसी द्वि-जीवन प्रकृति के आधार पर पड़ा है।
- विश्व में उभयचरों की लगभग 8,000 से अधिक ज्ञात प्रजातियाँ हैं, जिनमें मुख्यतः मेंढक, टोड, सलामैंडर और सीसिलियन (Caecilians) शामिल होते हैं।
- भारत में 430 से अधिक प्रजातियाँ दर्ज की जा चुकी हैं, जिनमें से अधिकांश एंडेमिक हैं, विशेषकर वेस्टर्न घाट और पूर्वोत्तर हिमालयी क्षेत्र में।
- उभयचर पर्यावरणीय परिवर्तनों के प्रति अत्यंत संवेदनशील होते हैं, इसलिए इन्हें “bio-indicators” माना जाता है।
उभयचरों की प्रमुख विशेषताएँ:
-
द्वि-जीवन (Dual Life Cycle): उभयचर अपने जीवन की शुरुआत लार्वा अवस्था में जल में करते हैं और वयस्क अवस्था में अधिकांशतः स्थल पर रहते हैं। इस कारण इनका जीवन-चक्र रूपांतरण (metamorphosis) पर आधारित होता है।
-
त्वचा के माध्यम से श्वसन (Cutaneous Respiration): इनकी त्वचा पतली, नम और ग्रंथियों से भरपूर होती है, जिसके माध्यम से गैसों का आदान-प्रदान होता है।
-
ठंडे-खून वाले जीव (Cold-Blooded / Ectothermic): इनका शरीर तापमान बाहरी वातावरण पर निर्भर करता है। इसलिए ये तापमान-संवेदनशील होते हैं और जलवायु परिवर्तन से गहरे प्रभावित होते हैं।
-
अंडे बिना खोल के (Non-Amniotic Eggs): उभयचर अंडों पर कठोर खोल नहीं होता। वे जेल जैसी संरचना में रहते हैं, जिन्हें सुरक्षित रखने के लिए जल या नम स्थान अनिवार्य होता है।
-
उच्च जैव-विविधता और स्थानिकता (High Endemism): भारतीय उपमहाद्वीप विशेष रूप से पश्चिमी घाट और पूर्वोत्तर क्षेत्रों में अत्यधिक एंडेमिक उभयचर पाए जाते हैं, जो स्थानीय पारिस्थितिकी के स्वास्थ्य का संकेतक होते हैं।
उभयचर प्रजातियों का महत्व:
-
पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखना: उभयचर कीटों की बड़ी मात्रा खाते हैं, जिससे कृषि और प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्रों में कीट-नियंत्रण होता है। इनके लार्वा जलीय तंत्र की ऊर्जा-श्रृंखला में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
-
जैव-संकेतक (Bio-indicators) के रूप में भूमिका: चूँकि उभयचर प्रदूषण, तापमान, रसायनों और रोगों के प्रति बेहद संवेदनशील हैं, इसलिए इनकी उपस्थिति या कमी किसी क्षेत्र के पर्यावरणीय स्वास्थ्य का संकेत देती है।
-
चिकित्सा और वैज्ञानिक अनुसंधान में उपयोग: कुछ उभयचरों का विष (skin toxins) औषधीय शोध में उपयोग होता है। कई पेप्टाइड्स कैंसर, उच्च रक्तचाप और संक्रमण के उपचार की में सहायक हैं। मेंढकों के भ्रूण विकास का अध्ययन जीव विज्ञान में महत्वपूर्ण है।
-
खाद्य-श्रृंखला का महत्वपूर्ण हिस्सा: उभयचर स्वयं कई शिकारी प्रजातियों—जैसे साँप, पक्षी और स्तनधारियों—के भोजन का प्रमुख स्रोत हैं। इनकी कमी खाद्य-श्रृंखला के टूटने का जोखिम बढ़ाती है।
-
जलवायु परिवर्तन की निगरानी: विश्व स्तर पर उभयचरों की तेजी से घटती जनसंख्या IPBES और IUCN की रिपोर्टों में जलवायु परिवर्तन, भूमि-उपयोग परिवर्तन और प्रदूषण के बढ़ते प्रभाव की पुष्टि करती है। इसलिए संरक्षण नीतियों में उभयचरों की स्थिति को प्रमुख संकेतक माना जाता है।