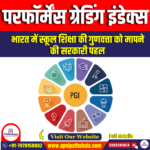चर्चा में क्यों?
भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) की मौद्रिक नीति समिति की 52वीं बैठक में प्रमुख नीतिगत दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया। रेपो दर को 6.50% पर स्थिर रखा गया, जबकि नकद आरक्षित अनुपात (CRR) में 50 आधार अंकों की कटौती कर इसे 4% किया गया।
आरबीआई एमपीसी बैठक (दिसंबर 2024) के मुख्य बिंदु:
- रेपो रेट: रेपो दर को 5% पर स्थिर रखा गया, जो फरवरी 2023 से अब तक बिना किसी बदलाव के है।
- यह लगातार 11वीं बार है जब ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
- सीआरआर कटौती: नकद आरक्षित अनुपात (CRR) को 50 बेसिस पॉइंट यानी 50% से घटाकर 4% किया गया, जिससे बैंकों को अतिरिक्त नकदी प्रवाह में मदद मिलेगी।
- मुद्रास्फीति का प्रभाव: आरबीआई ने महंगाई बढ़ने की संभावना जताई, जिससे आर्थिक विकास दर पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।
- इसी कारण GDP वृद्धि दर FY25 के लिए 2% से घटाकर 6.6% कर दी गई है।
- जीडीपी वृद्धि अनुमान:
- FY25 की पहली तिमाही में 9% और दूसरी तिमाही में 7.3% वृद्धि का अनुमान लगाया गया है।
- FY25 में समग्र GDP वृद्धि दर को 6% तक सीमित रखा गया।
- मुद्रास्फीति का अनुमान: FY25 के लिए मुद्रास्फीति दर को 8% पर रखा गया है, जबकि FY26 Q1 और Q2 के लिए यह क्रमशः 4.6% और 4% रहने की उम्मीद है।
- डिजिटल सुरक्षा: डिजिटल फ्रॉड को रोकने के लिए AI जैसे आधुनिक उपकरण पेश किए गए हैं।
- यूपीआई सेवा का विस्तार: यूपीआई सेवाएं अब छोटे वित्तीय बैंकों (Small Finance Banks) तक विस्तारित की जाएंगी, जिससे डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा मिलेगा।
- किसानों के लिए विशेष राहत:
- कोलेटरल फ्री एग्रीकल्चरल लोन (बिना गिरवी रखे कृषि ऋण) की सीमा को 6 लाख रुपए से बढ़ाकर 2 लाख रुपए प्रति उधारकर्ता किया गया।
- यह निर्णय कृषि लागत और महंगाई के बढ़ते स्तर को ध्यान में रखते हुए लिया गया।
- पिछली बार इसमें 2019 में बदलाव किया गया था।
- महत्वपूर्ण अन्य तथ्य:
- फरवरी 2023 में ब्याज दर में 25% की वृद्धि कर इसे 6.5% किया गया था।
- आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी बैठक हर दो महीने में आयोजित की जाती है।
- रिजर्व बैंक ने भविष्य की संभावित आर्थिक चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए नीतिगत रुख ‘तटस्थ’ बनाए रखने का निर्णय लिया है।
रेपो रेट क्या है?
रेपो रेट वह ब्याज दर है जिस पर देश का केंद्रीय बैंक (भारत में रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया) वाणिज्यिक बैंकों को धन की कमी होने पर ऋण देता है। यह दर मौद्रिक नीति को नियंत्रित करने का एक साधन है।
रेपो रेट का उपयोग:
- मुद्रास्फीति (Inflation) पर नियंत्रण:
- जब मुद्रास्फीति बढ़ती है, तो केंद्रीय बैंक रेपो रेट बढ़ा देता है।
- इससे वाणिज्यिक बैंकों के लिए केंद्रीय बैंक से ऋण लेना महंगा हो जाता है।
- परिणामस्वरूप, अर्थव्यवस्था में धन की आपूर्ति घटती है और मुद्रास्फीति पर नियंत्रण होता है।
- आर्थिक स्थिरता बनाए रखना: रेपो रेट में कमी से बैंकों को सस्ता ऋण मिलता है, जिससे अर्थव्यवस्था में धन का प्रवाह बढ़ता है और विकास को प्रोत्साहन मिलता है।
मुद्रास्फीति क्या है?
मुद्रास्फीति किसी विशेष अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में लगातार वृद्धि को कहते हैं। इससे उपभोक्ताओं की क्रय शक्ति घटती है, और नकदी का मूल्य कम हो जाता है।
मुद्रास्फीति को कौन मापता है?
भारत में सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) मुद्रास्फीति को मापता है।
मुद्रास्फीति के प्रमुख कारण:
- मांग में वृद्धि: जब वस्तुओं और सेवाओं की मांग आपूर्ति से अधिक हो जाती है।
- आपूर्ति में कमी: उत्पादन में बाधा या कच्चे माल की कमी से आपूर्ति घट जाती है।
- मांग-आपूर्ति का अंतर: मांग और आपूर्ति के बीच संतुलन का बिगड़ना।
- धन का अत्यधिक प्रचलन: जब अर्थव्यवस्था में धन की आपूर्ति जरूरत से अधिक होती है।
- इनपुट लागत में वृद्धि: कच्चे माल, बिजली, ईंधन आदि की कीमतों में वृद्धि।
- मुद्रा का अवमूल्यन: जब मुद्रा का मूल्य अंतरराष्ट्रीय बाजार में घटता है।
- मजदूरी में वृद्धि: श्रमिकों के वेतन में वृद्धि से उत्पादन लागत बढ़ती है।
मौद्रिक नीति समिति (MPC):
मौद्रिक नीति समिति (Monetary Policy Committee – MPC) भारत की आर्थिक नीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली एक वैधानिक संस्था है, जिसका उद्देश्य मुद्रास्फीति को नियंत्रित करते हुए आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है।
- गठन और पृष्ठभूमि
- MPC की स्थापना भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के बीच हुए समझौता ज्ञापन (MoU) के बाद की गई थी।
- इसका उद्देश्य मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण पर आधारित नई मौद्रिक नीति ढांचे को लागू करना है।
- रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 को वित्त अधिनियम, 2016 के माध्यम से संशोधित करके MPC को वैधानिक दर्जा दिया गया।
- कानूनी प्रावधान: संशोधित रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45ZB के तहत केंद्र सरकार को छह-सदस्यीय MPC गठित करने का अधिकार प्राप्त है।
- कार्य:
- MPC का मुख्य कार्य रेपो दर (Repo Rate) को निर्धारित करना है, ताकि मुद्रास्फीति को तय लक्ष्य के भीतर रखा जा सके।
- यह पहले की तकनीकी सलाहकार समिति (Technical Advisory Committee) की जगह कार्य करता है।
- संरचना
- MPC के छह सदस्य होते हैं:
- RBI गवर्नर (अध्यक्ष),
- मौद्रिक नीति संभालने वाले RBI के डिप्टी गवर्नर,
- RBI बोर्ड द्वारा नामित एक अधिकारी, और
- केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त तीन बाहरी सदस्य।
- बाहरी सदस्यों का कार्यकाल चार वर्षों का होता है।
- बैठक के लिए कोरम चार सदस्यों का होना आवश्यक है, जिनमें कम से कम एक RBI गवर्नर या उनकी अनुपस्थिति में डिप्टी गवर्नर होना चाहिए।
- निर्णय प्रक्रिया
- MPC के निर्णय बहुमत के आधार पर लिए जाते हैं।
- यदि वोटों में बराबरी होती है, तो RBI गवर्नर का निर्णायक वोट (Casting Vote) होता है।
- MPC के निर्णय RBI के लिए बाध्यकारी होते हैं।
- RBI की मौद्रिक नीति विभाग (MPD) MPC को नीति निर्धारण में सहयोग करती है।
मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी (Monetary Policy Committee):
- RBI की मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी हर दो महीने में बैठक करती है और ब्याज दरों को घटाने और बढ़ाने का फैसला करती है।
- इसका कार्य देश की अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करना है, और यह निर्णय देश के वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण होते हैं।
पॉलिसी रेट: पॉलिसी रेट (Policy Rate) किसी भी सेंट्रल बैंक का एक प्रभावी टूल है, जिसका उपयोग महंगाई को नियंत्रित करने और अर्थव्यवस्था में स्थिरता बनाए रखने के लिए किया जाता है।
महंगाई में पॉलिसी रेट का प्रभाव:
- महंगाई अधिक होने पर:
जब अर्थव्यवस्था में महंगाई बढ़ जाती है, तो सेंट्रल बैंक पॉलिसी रेट बढ़ाकर नकदी प्रवाह (Money Flow) को कम करता है।- पॉलिसी रेट बढ़ने पर बैंकों को सेंट्रल बैंक से कर्ज लेना महंगा पड़ता है।
- इसके परिणामस्वरूप, बैंक अपने ग्राहकों को दिए जाने वाले लोन पर ब्याज दरें बढ़ा देते हैं।
- ऊंची ब्याज दरों के कारण लोग और कंपनियां कम कर्ज लेती हैं, जिससे मांग में कमी आती है।
- डिमांड घटने से महंगाई में गिरावट आती है।
आर्थिक सुस्ती में पॉलिसी रेट का प्रभाव:
- अर्थव्यवस्था में सुस्ती के दौरान:
जब अर्थव्यवस्था कमजोर होती है और रिकवरी की आवश्यकता होती है, तो सेंट्रल बैंक पॉलिसी रेट घटा देता है।- इससे बैंकों को सेंट्रल बैंक से सस्ता कर्ज मिलने लगता है।
- बैंकों द्वारा ग्राहकों को कम ब्याज दरों पर लोन प्रदान किया जाता है।
- सस्ती दरों पर लोन मिलने से नकदी प्रवाह (Money Flow) बढ़ता है, जिससे मांग में वृद्धि होती है और अर्थव्यवस्था पुनर्जीवित होती है।
रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) के बारे में जानकारी:
- स्थापना:
- RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी।
- पहले यह भारतीय बैंकों के लिए मुद्रा और क्रेडिट की आपूर्ति को नियंत्रित करता था।
- मुख्यालय:
- RBI का हेडऑफिस पहले कोलकाता में था, लेकिन 1937 में इसे मुंबई स्थानांतरित कर दिया गया।
- 1949 में भारत सरकार ने RBI को पूरी तरह से अपने नियंत्रण में लिया।
- गवर्नर:
- RBI का सबसे बड़ा अधिकारी गवर्नर होता है, जो भारतीय बैंकिंग प्रणाली के लिए जिम्मेदार होता है।
- यह भारतीय बैंकों को लाइसेंस जारी करने का कार्य भी करता है, और विदेशों में भारतीय बैंकों के संचालन की निगरानी करता है।
- गवर्नर का कार्यकाल:
- RBI के गवर्नर का कार्यकाल 3 साल का होता है, लेकिन इसे बढ़ाया भी जा सकता है।
- इसका कार्यकाल सबसे अधिक 2754 दिन (जुलाई 1949 से 14 जनवरी 1957 तक) का था।
- अमिताव घोष ने 1985 में 20 दिन के लिए गवर्नर का कार्यभार संभाला था।
- पहला गवर्नर:
- RBI का पहला गवर्नर सर ऑस्कर सिम्स था।
- वर्तमान में शक्तिकांत दास RBI के गवर्नर है।
- गवर्नर की नियुक्ति:
- RBI के गवर्नर की नियुक्ति भारत सरकार करती है, जो वित्त मंत्रालय के मार्गदर्शन में होती है।
- गवर्नर की नियुक्ति केंद्रीय मंत्रिमंडल के अनुमोदन से की जाती है।
- आधिकारिक कार्य:
- RBI के गवर्नर का कार्य भारत के बैंकिंग क्षेत्र को नियंत्रित करना है, और यह सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए जिम्मेदार है।
- RBI के कार्यों में देश की वित्तीय नीति का निर्माण, मुद्रा आपूर्ति का नियंत्रण और बैंकिंग सेक्टर की स्थिरता बनाए रखना शामिल है।
- आधुनिक युग में योगदान: RBI अब वित्तीय क्षेत्र के नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और भारतीय बैंकिंग सिस्टम को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए कई सुधारों का कार्य करता है।
Explore our Books: https://apnipathshala.com/product-category/books/
Explore Our test Series: https://tests.apnipathshala.com/