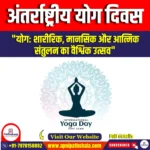GS Paper III: वित्तीय नीति, संसाधनों का जुटाव, निवेश मॉडल, समावेशी विकास |
चर्चा में क्यों?
भारतीय रेल बजट: हाल ही में, रेलवे बजट 2025 का ऐलान किया गया, जिसमें कुल ₹2.65 लाख करोड़ का आवंटन किया गया है। इस बजट का मुख्य फोकस पूंजीगत व्यय और इंफ्रास्ट्रक्चर विस्तार पर है। इस बजट में ग्राहक सुविधाओं और लोक क्षेत्र निवेश के लिए आवंटन में कमी हुई है।
भारतीय रेल बजट 2025 के मुख्य बिंदु
- रेलवे के लिए आवंटन: केंद्रीय बजट 2025 में भारतीय रेलवे के लिए ₹2.65 लाख करोड़ का आवंटन किया गया है, जिसमें से ₹2.52 लाख करोड़ सकल बजटीय समर्थन के रूप में और ₹10,000 करोड़ अतिरिक्त बजटीय संसाधनों से होंगे। इस बजट में पूंजीगत व्यय (Capex) को बढ़ाकर ₹2.62 लाख करोड़ किया गया है, जिसका उद्देश्य संपत्तियों का आधुनिकीकरण, इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार और सुरक्षा उपायों को बढ़ाना है।
- विकास: भारतीय रेलवे अगले 2–3 वर्षों में 200 नई वंदे भारत ट्रेनों, 100 अमृत भारत ट्रेनों, और 50 नमो भारत तेज़ रेल ट्रेनों को पेश करने की योजना बना रही है। इसके अलावा, 17,500 सामान्य गैर-एसी कोचों को जोड़ा जाएगा, जिससे निम्न और मध्यम आय वर्ग के यात्रियों के यात्रा अनुभव में सुधार होगा।
- सुरक्षा और स्थिरता: ₹1.16 लाख करोड़ रेलवे सुरक्षा परियोजनाओं के लिए आवंटित किए गए हैं, जिसमें उन्नत सुरक्षा प्रणालियाँ शामिल हैं। रेलवे का लक्ष्य 2025–26 तक 100% विद्युतीकरण पूरा करना है और इसके लिए छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर (SMRs) को गैर-जीवाश्म ऊर्जा स्रोत के रूप में अपनाने की योजना है।
- माल परिवहन और उच्च गति नेटवर्क: भारतीय रेलवे विश्व का दूसरा सबसे बड़ा माल परिवहनकर्ता बनने की दिशा में अग्रसर है, जिसका लक्ष्य इस वित्तीय वर्ष के अंत तक 1.6 बिलियन टन माल परिवहन करना है। इसके अलावा, 7,000 किमी लंबा उच्च गति रेल नेटवर्क बनाने की योजना है, जो 250 किमी प्रति घंटा तक की गति को सपोर्ट करेगा, और इसे 2047 तक पूरा करने का लक्ष्य है।
- रोजगार सृजन: बजट में रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश के माध्यम से रोजगार के अवसर उत्पन्न करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। साथ ही, मध्यम वर्ग को आयकर में राहत दी गई है, जो सरकार के विकसित भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप है।
- वित्तीय प्रावधान: राष्ट्रीय परियोजनाओं के लिए बाजार उधारी पर ऋण सेवा के लिए ₹706 करोड़ और निर्भया फंड से ₹200 करोड़ आवंटित किए गए हैं। रणनीतिक लाइनों पर परिचालन में हुए घाटे की भरपाई के लिए ₹2,739 करोड़ का आवंटन किया गया है। इसके अलावा, सकल बजटीय समर्थन 2013–14 के मुकाबले अब लगभग नौ गुना बढ़ गया है।
भारतीय रेलवे बजट का परिचय
- भारतीय रेलवे बजट देश के विशाल रेलवे नेटवर्क के लिए एक वार्षिक वित्तीय रिपोर्ट है, जिसे रेलवे बोर्ड द्वारा प्रबंधित किया जाता था।
- परंपरागत रूप से, यह बजट संसद में रेल मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जाता था, जो आमतौर पर केंद्रीय बजट से कुछ दिन पहले पेश किया जाता था।
- पहले, रेलवे मंत्री अगले वित्तीय वर्ष के लिए बजट अनुमान प्रस्तुत करते थे, साथ ही पिछले वर्ष की रेलवे गतिविधियों का प्रदर्शन भी बताया जाता था।
- 2016 के बाद, मोदी सरकार ने रेलवे बजट को सामान्य बजट में मिला शामिल कर लिया है। अब रेलवे बजट वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जाता है।
- यह बजट आगामी वर्ष के लिए प्राथमिकताएँ तय करने से संबंधित होता हैं। ये प्राथमिकताएँ अक्सर रेलवे नेटवर्क के विस्तार, रेल इन्फ्रास्ट्रक्चर में सुधार, और रेल परिवहन के लिए उपयोग होने वाले रोलिंग स्टॉक (ट्रेन और अन्य वाहन) में निवेश पर केंद्रित होती है।
रेलवे बजट का इतिहास
- शुरुआत: रेलवे बजट को पहली बार 1924 में सामान्य बजट से अलग किया गया था। यह निर्णय ब्रिटिश अर्थशास्त्री विलियम अकवर्थ की अध्यक्षता में बनी अकवर्थ समिति की सिफारिश के बाद लिया गया था। समिति ने भारतीय रेलवे के पुनर्गठन की सिफारिश भी की थी। इसके बाद से रेलवे बजट एक स्वतंत्र वित्तीय दस्तावेज बन गया, जिसे केंद्रीय बजट से कुछ दिन पहले प्रस्तुत किया जाता था। यह परंपरा 92 वर्षों तक जारी रही।
- पहला रेलवे बजट: भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद, पहला रेलवे बजट 1947 में देश के पहले रेलवे मंत्री जॉन माथाई द्वारा प्रस्तुत किया गया। यह एक नए युग की शुरुआत थी, जब देश अपने रेलवे सिस्टम को फिर से बनाना और विस्तार करना शुरू कर रहा था।
- विलय: 2016 में, मोदी सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया। जिसके तहत रेलवे बजट को सामान्य बजट में मिला दिया। यह निर्णय बेहतर वित्तीय एकीकरण और कार्यकुशलता की दिशा में एक कदम माना गया।
- विलय का तरीका: नए सिस्टम के तहत, वित्त मंत्रालय एक ही अनुमान विधेयक तैयार करता है, जिसमें रेलवे क्षेत्र के लिए अनुमानित बजट शामिल होता हैं।
- इसके तहत भारतीय रेलवे को सरकार को लाभांश देने की आवश्यकता नहीं थी, और इसका पूंजी ऋण भी समाप्त कर दिया गया था।
- इसी के साथ, रेलवे मंत्रालय को अपनी पूंजीगत व्यय को कवर करने के लिए वर्तमान में वित्त मंत्रालय से सकल बजट समर्थन प्राप्त होता है।
- प्रमुख रेलवे मंत्री:
- लालू प्रसाद यादव 2004 से 2009 तक रेलवे मंत्री रहे और उन्होंने छह बार रेलवे बजट प्रस्तुत किया।
- ममता बनर्जी 1999 में पहली महिला रेलवे मंत्री बनीं और 2000 में रेलवे बजट प्रस्तुत करने वाली पहली महिला बनीं।
- 2014 में, डी. वी. सदानंद गौड़ा ने रेलवे मंत्री के रूप में भारत की पहली बुलेट ट्रेन और उच्च गति वाली रेल मार्गों की शुरुआत की घोषणा की।
- केंद्रीय बजट से अलग अंतिम रेलवे बजट 25 फरवरी 2016 को सुरेश प्रभु द्वारा प्रस्तुत किया गया था।
रेलवे बजट की संरचना और प्रक्रिया
- संरचना
- रेलवे बजट को सुव्यवस्थित तरीके से प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें प्राप्तियों और व्ययों का स्पष्ट विभाजन होता है। यह भारतीय रेलवे की वित्तीय स्थिति का विस्तृत विवरण प्रदान करता है और यह दर्शाता है कि विभिन्न उद्देश्यों के लिए धन का आवंटन कैसे किया जाएगा।
- प्राप्तियां: इसमें यात्री किराया, मालभाड़ा, निवेश, और अन्य स्रोतों से आय शामिल होती है।
- व्यय: इसमें पूंजीगत व्यय (इन्फ्रास्ट्रक्चर, रोलिंग स्टॉक, आदि के लिए) और राजस्व व्यय (ऑपरेशनल लागत जैसे वेतन, रखरखाव, और सेवाएं) शामिल होते हैं।
- बजट को डिमांड्स फॉर ग्रांट्स और एप्रोप्रियेशन के रूप में बांटा जाता है, और इसमें विभिन्न वित्तीय दस्तावेज होते हैं।
- रेलवे के लिए धन के स्रोत: रेलवे के लिए धन विभिन्न स्रोतों से आता है, जिनमें प्रमुख रूप से संविधान सभा कोष और आपातकालीन कोष शामिल हैं।
- बजट तैयारी की प्रक्रिया
- तैयारी की प्रक्रिया नवंबर में शुरू होती है और फरवरी में बजट संसद में प्रस्तुत किए जाने के साथ समाप्त होती है।
- अनुमान: रेलवे प्रशासन विभिन्न इकाइयों और विभागों के साथ मिलकर आगामी वर्ष के लिए अपने वित्तीय आवश्यकताओं का अनुमान तैयार करता है। ये अनुमान पिछले वर्ष के वास्तविक व्यय और वर्तमान वर्ष के पहले सात महीनों के व्यय के आधार पर तैयार किए जाते हैं।
- समीक्षा: रेलवे मंत्रालय बदलती परिस्थितियों के मद्देनजर बजट आवश्यकताओं का मूल्यांकन करता है। मंत्रालय विशेष परिस्थितियों जैसे प्राकृतिक आपदाओं, सुरक्षा उपायों को भी ध्यान में रखता है।
- प्रस्तुति: रेलवे बोर्ड तैयारी प्रक्रिया में केंद्रीय भूमिका निभाता है। संशोधित और बजट अनुमान तैयार किए जाते हैं और बोर्ड के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किए जाते हैं।
- वित्तीय आयुक्त की समीक्षा: रेलवे के वित्तीय आयुक्त अनुमानों की समीक्षा करते हैं ताकि उनकी सटीकता और व्यवहार्यता सुनिश्चित हो सके। इसमें राजस्व और पूंजीगत व्यय की विस्तृत जांच की जाती है।
- वित्तीय दस्तावेज़: एक बार अनुमान अंतिम रूप से तैयार हो जाने पर विभिन्न दस्तावेज तैयार किए जाते हैं। डिमांड्स फॉर ग्रांट्स वह औपचारिक अनुरोध होते हैं जो संसद से किए जाते हैं।
- अंतिम रूप से प्रस्तुत करना: फरवरी में, अंतिम बजट वित्त मंत्री द्वारा संसद में प्रस्तुत किया जाता है।
- तैयारी की प्रक्रिया नवंबर में शुरू होती है और फरवरी में बजट संसद में प्रस्तुत किए जाने के साथ समाप्त होती है।
रेलवे बजट को सामान्य केंद्रीय बजट में मिलाने के कारण
- रेलवे राजस्व में गिरावट: 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद, रेलवे से प्राप्त राजस्व राष्ट्रीय आय में अन्य स्रोतों की तुलना में कहीं अधिक योगदान देता था। 1970 के दशक में रेलवे का राजस्व कुल राष्ट्रीय आय का लगभग 30% था, जबकि 2015-16 तक यह घटकर कुल राजस्व का सिर्फ 11.5% रह गया। इस गिरते योगदान ने रेलवे बजट को केंद्रीय बजट में मिलाने पर जोर दिया।
- प्रशासनिक जटिलताएं: रेलवे बजट और सामान्य बजट के अलग-अलग होने से प्रशासनिक जटिलताएं उत्पन्न हो रही थीं। इसके कारण राष्ट्रीय वित्त के प्रबंधन में बाधा उत्पन्न हुई, जिससे वित्तीय योजना और अनुमोदन के लिए समानांतर प्रणालियों की आवश्यकता महसूस की गई।
- आर्थिक दृष्टिकोण में बदलाव: पहले रेलवे बजट को अलग रखने का उद्देश्य रेलवे को वित्तीय स्वायत्तता प्रदान करना था। लेकिन जैसे-जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था विकसित हुई, रेलवे के लिए एक अलग वित्तीय संरचना बनाए रखने का विचार कम व्यवहारिक लगने लगा।
रेलवे बजट का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव
- बुनियादी ढांचे के विकास में वृद्धि: भारतीय रेलवे देश के बुनियादी ढांचे के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है। वार्षिक रेलवे बजट के माध्यम से रेलवे नेटवर्क के विस्तार, स्टेशनों का आधुनिकीकरण, यात्री और मालवाहन सेवाओं के विस्तार जैसे परियोजनाओं के लिए धन आवंटित किया जाता है।
- रोजगार सृजन: रेलवे भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता है। रेलवे बजट में किए गए निवेशों से इंजीनियरिंग, रखरखाव, और प्रशासन जैसे विभिन्न क्षेत्रों में लाखों रोजगार के अवसर उत्पन्न होते हैं। रेलवे नेटवर्क का विस्तार स्थानीय क्षेत्रों में भी रोजगार पैदा करता है।
- क्षेत्रीय विकास: नई रेल लाइनों की शुरुआत और मौजूदा नेटवर्क के उन्नयन ने विशेष रूप से दूरदराज और पिछड़े क्षेत्रों में क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा दिया है। जो क्षेत्र रेलवे से अच्छे से जुड़े होते हैं, वहां बेहतर बाजारों, रोजगारों और आवश्यक सेवाओं की पहुँच के कारण आर्थिक विकास होता है।
- व्यापार और वाणिज्य: भारतीय रेलवे देशभर में माल की ढुलाई (जैसे कोयला, कच्चे माल, कृषि उत्पाद और तैयार माल) में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। रेलवे बजट में अक्सर मालवाहन क्षमता को बढ़ाने के लिए धन आवंटित किया जाता है, जो सीधे तौर पर औद्योगिक और कृषि क्षेत्रों पर प्रभाव डालता है।
- पर्यटन: रेलवे प्रणाली ने देशभर में प्रमुख पर्यटक स्थलों तक पहुँच में सुधार करके पर्यटन के क्षेत्र में भी अहम भूमिका निभाई है। पर्यटक ट्रेनों का विकास, उदाहरण स्वरूप, घरेलू और अंतरराष्ट्रीय पर्यटन से राजस्व लाता है, जो सेवा क्षेत्र को और बढ़ावा देता है।
यूपीएससी पिछले वर्षों के प्रश्न (PYQs) प्रश्न (2015): भारतीय रेलवे द्वारा उपयोग किए गए बायो-टॉयलेट्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही हैं? (a) केवल 1 प्रश्न (2023): दुनिया के विभिन्न देशों में रेलवे के परिचय के सामाजिक-आर्थिक प्रभावों को स्पष्ट करें। |
Explore our Books: https://apnipathshala.com/product-category/books/
Explore Our test Series: https://tests.apnipathshala.com/