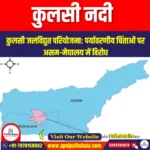संदर्भ:
कॉलेजियम प्रणाली: उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने राज्यसभा के फ्लोर नेताओं के साथ बैठक की, जिसमें दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस यशवंत वर्मा के आवास से बरामद अर्ध–जले भारतीय करेंसी नोटों के मामले पर चर्चा की गई।
भारत में न्यायाधीशों की नियुक्ति:
पृष्ठभूमि
- भारत में न्यायाधीशों की नियुक्ति को लेकर पारदर्शिता, जवाबदेही और न्यायिक स्वतंत्रता से जुड़े मुद्दों पर व्यापक बहस होती रही है।
- उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए दो प्रमुख प्रणालियाँ अपनाई गई हैं – कॉलेजियम प्रणाली (Collegium System) और राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJAC)।
- वर्तमान कॉलेजियम प्रणाली को अपारदर्शिता और औपचारिक प्रक्रियाओं की कमी के कारण आलोचना झेलनी पड़ती है, जबकि NJAC को सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक स्वतंत्रता के उल्लंघन के आधार पर रद्द कर दिया था।
संवैधानिक प्रावधान (Judicial Appointment in India):
- अनुच्छेद 124:
- सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
- राष्ट्रपति, उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय के ऐसे न्यायाधीशों से परामर्श ले सकते हैं, जिन्हें वह आवश्यक समझें।
- मुख्य न्यायाधीश (CJI) की नियुक्ति को छोड़कर, अन्य सभी न्यायिक नियुक्तियों में CJI से परामर्श अनिवार्य है।
- अनुच्छेद 217:
- उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
- इसमें मुख्य न्यायाधीश (CJI), राज्य के राज्यपाल, और संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लिया जाता है।
कॉलेजियम प्रणाली (Collegium System):
- सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण की एक प्रक्रिया है।
- यह प्रणाली संविधान में स्पष्ट रूप से उल्लेखित नहीं है बल्कि “जजेस केस” (Judges Cases) के न्यायिक निर्णयों के माध्यम से विकसित हुई।
- इस प्रणाली में न्यायपालिका को अपने ही सदस्यों को चुनने की प्राथमिकता दी गई है, जिससे कार्यपालिका (Executive) की भूमिका सीमित हो जाती है।
कॉलेजियम प्रणाली की संरचना:
- सुप्रीम कोर्ट के लिए– मुख्य न्यायाधीश (CJI) और सुप्रीम कोर्ट के चार वरिष्ठतम न्यायाधीश।
- उच्च न्यायालय के लिए– संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और दो वरिष्ठतम न्यायाधीश।
- कॉलेजियम द्वारा दी गई सिफारिशें सरकार को भेजी जाती हैं।
- सरकार स्पष्टीकरण मांग सकती है या जाँच (Intelligence Bureau – IB) करवा सकती है।
- यदि कॉलेजियम अपनी सिफारिश दोहराता है, तो सरकार को उसे स्वीकार करना अनिवार्य होता है।
कॉलेजियम प्रणाली की आलोचनाएँ:
- अपारदर्शिता (Lack of Transparency)– इस प्रणाली में कोई आधिकारिक तंत्र या सचिवालय (Secretariat) नहीं है, जिससे नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी नहीं रहती।
- निर्धारित पात्रता मानदंडों की अनुपस्थिति– न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कोई निर्धारित योग्यता मानदंड (Eligibility Criteria) या स्पष्ट चयन प्रक्रिया नहीं है।
- गोपनीय निर्णय प्रक्रिया– निर्णय बंद दरवाजों के पीछे लिए जाते हैं, और कॉलेजियम बैठकों का कोई सार्वजनिक रिकॉर्ड या कार्यवृत्त (Minutes) उपलब्ध नहीं होता।
- वकीलों की अनभिज्ञता – अधिवक्ता (Lawyers) अक्सर यह नहीं जान पाते कि उनके नाम न्यायिक नियुक्तियों के लिए विचाराधीन हैं या नहीं।