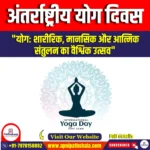सामान्य अध्ययन पेपर II: पारदर्शिता और जवाबदेहिता, सरकारी नीतियाँ और हस्तक्षेप, महत्त्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थान |
चर्चा में क्यों?
भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024: हाल ही में, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने 2024 का भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक (CPI) जारी किया है, जिसमें यह सामने आया कि अधिकांश देशों ने सार्वजनिक क्षेत्र में भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए कम या कोई प्रगति नहीं की है। यह भ्रष्टाचार पर नियंत्रण की वैश्विक चुनौतियों को उजागर करता है।
भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 (CPI) के मुख्य बिंदु:
- CPI 2024 में 180 देशों और क्षेत्रों को सार्वजनिक क्षेत्र में भ्रष्टाचार के स्तर के आधार पर रैंक किया गया है।
- इस सूचकांक में 13 स्वतंत्र डेटा स्रोतों का उपयोग किया गया है।
- पैमाना: इसे 0 से 100 तक की पैमाने पर मापा गया है। 0 का मतलब है अत्यधिक भ्रष्टाचार और 100 का मतलब है अत्यधिक पारदर्शिता और ईमानदारी।
- शीर्ष स्थान: 2024 के CPI में डेनमार्क (90), फिनलैंड (88), और सिंगापुर (84) शीर्ष स्थानों पर रहे हैं। ये देश पारदर्शिता और भ्रष्टाचार पर नियंत्रण में वैश्विक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं।
- निचला स्थान: इस सूचकांक में दक्षिण सूडान (8), सोमालिया (9), और वेनेजुएला (10) जैसे देश सूचकांक के निचले स्थान में हैं, जो भ्रष्टाचार के उच्चतम स्तर को दर्शाते हैं।
- भारत: CPI 2024 में भारत 180 देशों में से 96वें स्थान पर है। भारत का कुल स्कोर 38 है, जो 2023 में 39 और 2022 में 40 था।
- भारत के पड़ोसी देश: भारत के पड़ोसी देशों में, पाकिस्तान 135वें स्थान पर, श्रीलंका 121वें स्थान पर और बांग्लादेश 149वें स्थान पर रहा। चीन ने तुलनात्मक रूप से बेहतर प्रदर्शन करते हुए 76वां स्थान हासिल किया।
- निष्कर्ष:
- सूचकांक के अनुसार कुछ देशों में मजबूत, स्वतंत्र संस्थान और मुक्त, निष्पक्ष चुनाव हुए हैं, जबकि अन्य देशों में अत्यधिक सत्तावादी शासन है।
- CPI के अनुसार, दुनिया भर में देशों का औसत स्कोर 43/100 है अर्थात् अधिकांश देशों में भ्रष्टाचार की समस्या अभी भी गंभीर बनी हुई है।
- CPI के अनुसार, दो-तिहाई देशों का स्कोर 50 से कम है, जो यह दर्शाता है कि पारदर्शिता और भ्रष्टाचार पर नियंत्रण में बड़े सुधार की आवश्यकता है।
- CPI 2024 सूचकांक में 32 देशों ने अपनी रेटिंग में सुधार किया जबकि 47 देशों में भ्रष्टाचार में वृद्धि हुई है।
भ्रष्टाचार का अर्थव्यवस्था, जनजीवन और समाज पर प्रभाव
- अर्थव्यवस्था पर प्रभाव: भ्रष्टाचार के कारण व्यापारिक माहौल प्रभावित होता है, जिससे नए व्यवसाय शुरू करने में कठिनाई होती है। रिश्वतखोरी और अनावश्यक लालफीताशाही (अत्यधिक प्रशासनिक प्रक्रियाएँ) व्यवसायों की लागत बढ़ा देती हैं और विदेशी निवेशकों को हतोत्साहित करती हैं। इसके परिणामस्वरूप, कई विदेशी कंपनियाँ भ्रष्टाचार-प्रभावित देशों में निवेश करने से बचती हैं, जिससे आर्थिक विकास धीमा पड़ जाता है।
- समाज पर प्रभाव: भ्रष्टाचार के चलते लोग सरकार पर विश्वास खो देते हैं, जिससे लोकतांत्रिक प्रणाली कमजोर होती है। यदि नेता भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाते हैं, तो लोग चुनावों में भाग लेने से हतोत्साहित होते हैं, जिससे “मतदाता उदासीनता” (Voter Apathy) बढ़ती है। धीरे-धीरे, समाज में भ्रष्टाचार एक सामान्य प्रक्रिया के रूप में स्वीकार किया जाने लगता है, जिससे नैतिक मूल्यों में गिरावट आती है और सुधार लाना और भी मुश्किल हो जाता है।
- जनजीवन पर प्रभाव: भ्रष्टाचार की वजह से सरकारी सेवाओं की गुणवत्ता प्रभावित होती है, जिससे आम नागरिकों को बुनियादी सुविधाओं के लिए भी रिश्वत देनी पड़ती है। नगरपालिकाओं, बिजली आपूर्ति, राहत कोष वितरण जैसी सेवाओं में भी पारदर्शिता की कमी होती है, जिससे केवल पैसे वाले लोग ही अच्छी सेवाएँ प्राप्त कर पाते हैं। न्याय प्रणाली में भ्रष्टाचार से अपराधियों को बच निकलने का अवसर मिलता है, जबकि निर्दोष लोगों को न्याय पाने के लिए सालों संघर्ष करना पड़ता है।
भ्रष्टाचार और जलवायु संकट
भ्रष्टाचार न केवल सामाजिक और आर्थिक ढांचे को कमजोर करता है, बल्कि यह जलवायु संकट को और भी जटिल बना देता है।
- जलवायु निधियों का दुरुपयोग: जलवायु अनुकूलन और शमन उपायों के लिए जो धन निर्धारित किया जाता है, वह भ्रष्टाचार द्वारा हड़प लिया जाता है। इससे जलवायु परिवर्तन से लड़ने वाले कार्यक्रमों का प्रभावी कार्यान्वयन नहीं हो पाता और निर्धारित धन सही स्थानों तक नहीं पहुँचता। जलवायु संकट से प्रभावित गरीब और कमजोर समुदायों को मदद नहीं मिल पाती, क्योंकि जो धन उन तक पहुँचना चाहिए था, वह भ्रष्टाचार के कारण फंस जाता है या गलत स्थानों पर उपयोग किया जाता है।
- व्यापारिक हितों का अत्यधिक प्रभाव: भ्रष्टाचार के कारण व्यावसायिक और कॉर्पोरेट हितों का दबाव बढ़ता है। इससे सही जलवायु नीति बनाने और लागू करने में कठिनाई होती है। ये हित न केवल नीति निर्माण को प्रभावित करते हैं, बल्कि कई बार जलवायु परिवर्तन से निपटने के प्रयासों को भी कमजोर कर देते हैं। बड़ी कंपनियाँ और उद्योग अपनी लाभकारी नीतियों को बढ़ावा देने के लिए भ्रष्टाचार का सहारा लेते हैं, जिससे जलवायु संकट से निपटने की प्रभावी नीतियाँ विकसित नहीं हो पातीं।
- विकृत जलवायु नीतियाँ: कई देशों में जहां भ्रष्टाचार का स्तर अधिक है, वहाँ जलवायु नीति निर्माण पारदर्शी नहीं होती। व्यावसायिक हितों के प्रभाव में नीति निर्माण विकृत हो जाता है, जिससे पर्यावरण की रक्षा के लिए सही कदम नहीं उठाए जा पाते।
- पर्यावरण कानूनों का कमजोर प्रवर्तन: अधिकारियों को रिश्वत देकर पर्यावरणीय उल्लंघनों को नजरअंदाज किया जाता है। यह भ्रष्टाचार पर्यावरण के लिए बहुत हानिकारक होता है, क्योंकि इससे पर्यावरणीय कानूनों का पालन सही तरीके से नहीं हो पाता। इस प्रकार का भ्रष्टाचार वैश्विक पर्यावरणीय अपराधों को बढ़ावा देता है, जैसे कि अवैध वनों की कटाई, वन्यजीवों का शिकार आदि। वर्तमान में यह अब चौथा सबसे बड़ा संगठित अपराध बन चुका है।
जलवायु संकट से निपटने के लिए भ्रष्टाचार पर नियंत्रण
- जलवायु वित्त (Climate Finance) में पारदर्शिता बनाए रखना आवश्यक है ताकि संसाधनों का दुरुपयोग न हो। सरकारों और निजी क्षेत्र को अपने जलवायु संबंधी निवेशों और परियोजनाओं की जानकारी सार्वजनिक करनी चाहिए। सूचना का अधिकार (RTI) और स्वतंत्र ऑडिटिंग प्रक्रियाओं को मजबूत करना, ताकि जलवायु परियोजनाओं के क्रियान्वयन पर निगरानी बनी रहे।
- जलवायु संकट से निपटने के लिए सभी देशों को संयुक्त राष्ट्र, G20 और अन्य अंतरराष्ट्रीय मंचों पर समन्वय बनाना होगा। विकसित देशों को विकासशील देशों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करनी चाहिए, ताकि वे अपनी जलवायु नीतियों को प्रभावी रूप से लागू कर सकें। जलवायु समझौतों के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए स्वतंत्र पर्यवेक्षक संस्थाओं (Independent Oversight Bodies) का गठन किया जाना चाहिए।
- जलवायु परियोजनाओं में स्थानीय समुदायों को शामिल करना और उन्हें निगरानी की जिम्मेदारी देना भ्रष्टाचार को कम करने में सहायक होगा। प्रभावित समुदायों को जलवायु वित्त और परियोजनाओं की जानकारी उपलब्ध कराकर सामाजिक ऑडिट की प्रक्रिया को बढ़ावा देना चाहिए। ग्राम सभाओं, नागरिक संगठनों और पर्यावरण कार्यकर्ताओं की भूमिका को मजबूत कर उनके योगदान को मान्यता दी जानी चाहिए।
भारत में भ्रष्टाचार रोकने के उपाय
- विधायी उपाय (Legislative Measures): भ्रष्टाचार को रोकने के लिए भारत में कई कानून बनाए गए हैं, जो भ्रष्ट गतिविधियों की परिभाषा, दंड, और अवैध रूप से अर्जित संपत्ति की जब्ती से संबंधित प्रावधानों को निर्धारित करते हैं।
- भारतीय दंड संहिता, 1860 (Indian Penal Code, 1860): इसमें रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार से संबंधित कई धाराएँ शामिल हैं।
- भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (Prevention of Corruption Act, 1988): यह अधिनियम रिश्वत लेने और देने वालों के लिए कठोर दंड का प्रावधान करता है।
- मनी लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम, 2002 (Prevention of Money Laundering Act, 2002): भ्रष्टाचार से अर्जित धन को सफेद धन में बदलने की प्रक्रिया (मनी लॉन्ड्रिंग) को रोकने के लिए लागू किया गया।
- विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम, 2010 (Foreign Contribution Regulation Act, 2010): इसमें विदेशी चंदे के दुरुपयोग और राजनीतिक दलों या संगठनों में भ्रष्टाचार पर नियंत्रण के प्रावधान हैं।
- कंपनी अधिनियम, 2013 (Companies Act, 2013): इसमें कंपनियों में कॉर्पोरेट भ्रष्टाचार और अनियमितताओं को रोकने के प्रावधान किए गए हैं।
- लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 (Lokpal and Lokayuktas Act, 2013): यह अधिनियम उच्च पदों पर बैठे सरकारी अधिकारियों और नेताओं पर नजर रखने के लिए लागू किया गया।
- संस्थागत उपाय (Institutional Measures): भारत में भ्रष्टाचार पर नियंत्रण के लिए कई संस्थाएँ कार्यरत हैं, जो जाँच और निगरानी का कार्य करती हैं।
- केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC): यह स्वतंत्र निकाय सरकारी कार्यालयों में भ्रष्टाचार रोकने और सतर्कता बढ़ाने का कार्य करता है।
- केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI): यह देश की प्रमुख जांच एजेंसी है, जो उच्चस्तरीय भ्रष्टाचार के मामलों की जाँच करती है।
- नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG): यह सरकारी खर्चों का ऑडिट करता है और वित्तीय अनियमितताओं को उजागर करता है।
- केंद्रीकृत सार्वजनिक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (CPGRAMS): यह ऑनलाइन पोर्टल नागरिकों की शिकायतों को प्रभावी ढंग से हल करने के लिए बनाया गया है।
- तकनीकी उपाय (Technological Measures): डिजिटल प्रौद्योगिकी के माध्यम से पारदर्शिता बढ़ाकर और सरकारी अधिकारियों व जनता के बीच प्रत्यक्ष संपर्क को कम करके भ्रष्टाचार को रोकने के प्रयास किए जा रहे हैं।
- ई-गवर्नेंस (E-Governance): सरकारी सेवाओं को ऑनलाइन उपलब्ध कराकर निर्णय प्रक्रिया में पारदर्शिता लाई गई है।
- डिजिटल भुगतान (Digital Payments): भ्रष्टाचार को कम करने के लिए नगद लेन-देन को घटाकर डिजिटल भुगतान को बढ़ावा दिया गया है।
- ऑनलाइन सेवाएँ (Online Services): पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, सरकारी योजनाओं की सब्सिडी, और अन्य सेवाएँ ऑनलाइन उपलब्ध कराई जा रही हैं, जिससे बिचौलियों की भूमिका कम हुई है।
UPSC पिछले वर्षों के प्रश्न PYQs प्रश्न (2017): ‘बेनामी संपत्ति लेन-देन निषेध अधिनियम, 1988 (PBPT अधिनियम)’ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? (a) केवल 1 (b) केवल 2 (c) केवल 1 और 3 (d) केवल 2 और 3 उत्तर: (b) प्रश्न (2021): चर्चा कीजिये कि किस प्रकार उभरती प्रौद्योगिकियाँ और वैश्वीकरण मनी लॉन्ड्रिंग में योगदान करते हैं। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर मनी लॉन्ड्रिंग की समस्या से निपटने के लिये किये जाने वाले उपायों को विस्तार से समझाइये। |
Explore our Books: https://apnipathshala.com/product-category/books/
Explore Our test Series: https://tests.apnipathshala.com/