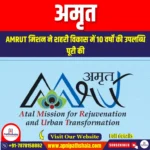सामान्य अध्ययन पेपर III: आपदा प्रबंधन, पर्यावरण प्रदूषण और गिरावट |
चर्चा में क्यों?
हाल ही में संसद द्वारा आपदा प्रबंधन (संशोधन) विधेयक 2024 पास किया गया है, जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों की कार्यप्रणाली को अधिक प्रभावी बनाना है। यह विधेयक राज्यों को आपदाओं से बेहतर ढंग से निपटने में सहायता प्रदान करेगा।
आपदा प्रबंधन (संशोधन) विधेयक 2024 की प्रमुख विशेषताएँ
- शहरी आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (UDMA) का गठन: विधेयक में राज्यों की राजधानियों और बड़े नगर निगम वाले शहरों में एक पृथक शहरी आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (Urban Disaster Management Authority) स्थापित करने का प्रावधान है। यह शहरी क्षेत्रों में आपदा से जुड़े खतरों को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने में सहायक होगा। हालांकि, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और केंद्रशासित प्रदेश चंडीगढ़ को इससे बाहर रखा गया है।
- राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (SDRF) का गठन: विधेयक राज्य सरकारों को राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (State Disaster Response Force – SDRF) बनाने की शक्ति प्रदान करता है। राज्य सरकार SDRF के कार्यों को परिभाषित करेगी और इसके सदस्यों की सेवा शर्तों को भी निर्धारित करेगी। यह बल आपदा के दौरान त्वरित प्रतिक्रिया सुनिश्चित करेगा।
- यह विधेयक आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 में संशोधन करने के लिए लाया गया है।
- आपदा प्रबंधन योजनाओं का निर्माण: संशोधन के तहत अब राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (SDMA) स्वयं आपदा प्रबंधन योजनाओं का निर्माण करेंगे। पहले यह कार्य राष्ट्रीय और राज्य कार्यकारी समितियों द्वारा किया जाता था।
- आपदा डेटाबेस का निर्माण: विधेयक राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर एक व्यापक आपदा डेटाबेस (Disaster Database) के निर्माण का प्रावधान करता है। यह डेटाबेस आपदा जोखिम आकलन, निधि आवंटन, व्यय प्रबंधन, आपदा पूर्व तैयारी और जोखिम रजिस्टर जैसे पहलुओं को समाहित करेगा।
- आपदा जोखिमों का आकलन: विधेयक में NDMA और SDMA को समय-समय पर आपदा जोखिमों का मूल्यांकन करने का दायित्व दिया गया है। इसमें जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न खतरों और अत्यधिक मौसम की घटनाओं जैसे नए जोखिमों का आकलन भी शामिल होगा। इससे आपदाओं का समय पर पूर्वानुमान लगाकर नुकसान को कम किया जा सकेगा।
- तकनीकी सहायता और दिशा-निर्देश: विधेयक के अनुसार NDMA और SDMA अपने अधीनस्थ निकायों को तकनीकी सहायता प्रदान करेंगे। साथ ही ये प्राधिकरण राहत और पुनर्वास के लिए न्यूनतम मानकों पर दिशा-निर्देश भी जारी करेंगे।
- विधेयक NDMA को नियम बनाने की शक्ति प्रदान करता है, लेकिन इसके लिए केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति आवश्यक होगी।
- राष्ट्रीय और उच्च स्तरीय समितियों को वैधानिक दर्जा: विधेयक में राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति (National Crisis Management Committee – NCMC) और उच्च स्तरीय समिति (High-Level Committee – HLC) को वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है।
- NCMC बड़े और राष्ट्रीय महत्व की आपदाओं को संभालने की नोडल संस्था के रूप में कार्य करेगी, जबकि HLC आपदा के दौरान राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी।
- नियुक्तियों का प्रावधान: विधेयक में NDMA को केंद्रीय सरकार की पूर्व अनुमति से अधिकारियों, कर्मचारियों, विशेषज्ञों और सलाहकारों की नियुक्ति का अधिकार दिया गया है।
आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005
|
आपदा प्रबंधन (संशोधन) विधेयक 2024 का मुख्य उद्देश्य
- संस्थागत संरचनाओं को सुदृढ़ बनाना: विधेयक का प्राथमिक उद्देश्य राष्ट्रीय और उप-राष्ट्रीय स्तर पर आपदा प्रबंधन संस्थाओं को अधिक जवाबदेह और सुस्पष्ट बनाना है। इससे आपदा प्रबंधन की प्रक्रियाएं अधिक संगठित होंगी और जिम्मेदारियों का स्पष्ट वितरण होगा, जिससे आपात स्थितियों में त्वरित निर्णय लिए जा सकेंगे।
- आपदा जोखिम मूल्यांकन में सुधार: इस विधेयक का एक प्रमुख उद्देश्य उभरते खतरों और जलवायु परिवर्तन से जुड़ी आपदाओं का समय-समय पर मूल्यांकन करना है। बढ़ती चरम मौसम घटनाओं के कारण आपदा प्रबंधन में सक्रिय दृष्टिकोण अपनाना आवश्यक हो गया है। यह संशोधन संस्थानों को नए जोखिमों की पहचान कर बेहतर योजना बनाने में सक्षम बनाएगा।
- विकेंद्रीकरण में सुधार: आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के कार्यान्वयन के दौरान राज्यों को कई संरचनात्मक चुनौतियों का सामना करना पड़ा। यह संशोधन राज्यों को अधिक अधिकार और संसाधन प्रदान करता है ताकि वे स्थानीय स्तर पर बेहतर निर्णय ले सकें और आपदा प्रबंधन में स्वायत्तता सुनिश्चित हो सके।
- वित्तीय संसाधनों का प्रबंधन: यह संशोधन आपदा प्रबंधन के लिए वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता और उपयोग में सुधार लाने पर बल देता है। राष्ट्रीय और राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (NDRF और SDRF) के प्रभावी उपयोग के साथ ही वित्तीय पारदर्शिता को प्राथमिकता दी गई है, जिससे राहत कार्य अधिक सुचारु होंगे।
- डेटा और प्रौद्योगिकी का एकीकरण: आपदा प्रबंधन में डेटा और प्रौद्योगिकी की भूमिका को सुदृढ़ करने पर विशेष जोर दिया गया है। विधेयक में एक समग्र आपदा डेटाबेस के निर्माण का प्रावधान है, जो आपदा पूर्व चेतावनी, वित्तीय व्यय, तैयारी और जोखिम आकलन को वास्तविक समय (Real-Time) पर ट्रैक करके आपदा प्रबंधन की गुणवत्ता में सुधार करने में सक्षम होगा।
आपदा प्रबंधन (संशोधन) विधेयक 2024 से संबंधित प्रमुख मुद्दे
- केंद्रीकरण की चिंता: विधेयक में केंद्र सरकार को नियम बनाने और विनियमन में व्यापक अधिकार देने पर आपत्ति जताई गई है। यह संघीय ढांचे को कमजोर करता है और राज्यों की स्वायत्तता पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। राज्यों की विशिष्ट आवश्यकताओं को समझने में देरी और केंद्रीकृत निर्णय लेने से राहत कार्य बाधित हो सकते हैं।
- वित्तीय विकेंद्रीकरण की कमी: शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) के लिए UDMA का गठन, उपकरणों की व्यवस्था और संचालन के लिए वित्तीय संसाधन जुटाना एक बड़ी चुनौती होगी। वित्तीय अधिकारों का केंद्रीकरण होने से आवश्यक संसाधनों की कमी आपदा प्रबंधन को बाधित कर सकती है, विशेष रूप से उन शहरों में जो वित्तीय रूप से कमजोर हैं।
- राज्यों के अधिकारों का अतिक्रमण: आपदा प्रबंधन और वित्तीय संसाधनों के उपयोग में राज्यों की भूमिका सीमित होने की संभावना है। कई विशेषज्ञों का मानना है कि यह विधेयक आपदा नियोजन में राज्यों के अधिकारों पर केंद्र का नियंत्रण बढ़ा सकता है, जिससे निर्णय लेने की प्रक्रिया में असमंजस और देरी हो सकती है।
- शहरी आपदा प्रबंधन में समन्वय की समस्या: विधेयक में शहरी आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (UDMA) के गठन का प्रावधान है, परंतु शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) की सीमित क्षमताओं पर सवाल उठाए जा रहे हैं। छोटे शहरों में जहाँ नगर आयुक्त जिला कलेक्टर की तुलना में कनिष्ठ होते हैं, वहां समन्वय की समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। संसाधनों का अभाव भी UDMA की प्रभावशीलता को प्रभावित कर सकता है।
- सीमित दायरा: विधेयक में आपदा की परिभाषा को विस्तृत नहीं किया गया है, जिससे हीटवेव (लू) और जलवायु परिवर्तन से प्रेरित अन्य आपदाओं को शामिल नहीं किया गया है। बढ़ते जलवायु खतरों के बीच, ऐसी घटनाओं को नजरअंदाज करना आपदा प्रबंधन की समग्रता को कमजोर कर सकता है।
- संवैधानिकता: विधेयक को सातवीं अनुसूची की समवर्ती सूची (Concurrent List) के प्रविष्टि 23 के तहत लाया गया है, जो “सामाजिक सुरक्षा और बीमा, रोजगार और बेरोजगारी” से संबंधित है। आपदा प्रबंधन का स्पष्ट उल्लेख सातवीं अनुसूची में नहीं है।
आपदा प्रबंधन से संबंधित महत्वपूर्ण पहल
- आपदा जोखिम न्यूनीकरण (Disaster Risk Reduction): आपदा जोखिम न्यूनीकरण का उद्देश्य नई आपदाओं को रोकना, मौजूदा जोखिम को कम करना और अवशिष्ट (बचे हुए) जोखिम का प्रभावी प्रबंधन करना है। बेहतर भूमि-उपयोग योजना, बाढ़-प्रतिरोधी संरचनाएं और जलवायु-सम्बंधित आपदाओं के प्रति जागरूकता फैलाना इसके प्रमुख उद्देश्य हैं।
- पूर्व-चेतावनी प्रणाली (Early Warning System): पूर्व-चेतावनी प्रणाली किसी भी आसन्न आपदा की जानकारी समय रहते प्रदान करती है, जिससे लोगों को सुरक्षित स्थान पर जाने और बचाव कार्य शुरू करने का अवसर मिलता है। भौगोलिक-आधारित मोबाइल अलर्ट और रडार तकनीक के माध्यम से तूफान, बाढ़, या भूकंप जैसी आपदाओं की पूर्व सूचना देना इस प्रणाली की अहम विशेषता है।
- क्षमता विकास (Capacity Building): आपदा प्रबंधन में स्थायी सफलता के लिए क्षमता विकास आवश्यक है। इसमें स्थानीय समुदायों, आपदा मित्र स्वयंसेवकों और सरकारी एजेंसियों को प्रशिक्षित कर आवश्यक कौशल और संसाधन प्रदान किए जाते हैं। आपदा प्रबंधन अभ्यास, खोज एवं बचाव अभियान, और जागरूकता कार्यक्रम इस प्रक्रिया का हिस्सा हैं, जो आपदा के दौरान त्वरित प्रतिक्रिया सुनिश्चित करते हैं।
UPSC पिछले वर्षों के प्रश्न (PYQs) प्रश्न (2020): आपदा प्रबंधन में पूर्ववर्ती प्रतिक्रियात्मक उपागम से हटते हुए भारत सरकार द्वारा आरंभ किये गए अभिनूतन उपायों की विवेचना कीजिये। प्रश्न (2016): राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एन.डी.एम.ए.) के सुझावों के संदर्भ में, उत्तराखंड के अनेकों स्थानों पर हाल ही में बादल फटने की घटनाओं के संघात को कम करने के लिये अपनाए जाने वाले उपायों पर चर्चा कीजिये। |
Explore our Books: https://apnipathshala.com/product-category/books/
Explore Our test Series: https://tests.apnipathshala.com/