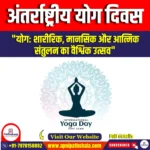सामान्य अध्ययन पेपर I: भौतिक भूगोल, भूकंप, आपदा प्रबंधन |
चर्चा में क्यों?
म्यांमार भूकंप 2025: 28 मार्च 2025 को म्यांमार के मध्य क्षेत्र में एक विनाशकारी भूकंप आया, जिससे मंडाले समेत कई इलाके प्रभावित हुए। इस त्रासदी में कई लोगों की जान गई और बुनियादी ढांचे को भी गंभीर नुकसान पहुंचा।
म्यांमार भूकंप 2025 से संबंधित जानकारी
- भूकंप की तीव्रता:
- इस भूकंप की तीव्रता 7.7 मापी गई, जो हाल के वर्षों में सबसे शक्तिशाली भूकंपों में से एक है।
- मुख्य भूकंप के 12 मिनट बाद 6.4 तीव्रता का एक और झटका महसूस किया गया।
- केंद्र:
- इसका केंद्र सागाइंग (Sagaing) शहर से 16 किलोमीटर उत्तर-पश्चिम में स्थित था।
- यह भूकंप भूसतह से 10 किलोमीटर की गहराई पर उत्पन्न हुआ।
- यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे (USGS) के अनुसार, यह एक अत्यंत उथला भूकंप था, जिससे सतह पर प्रभाव अधिक विनाशकारी हुआ।
- अधिकेंद्र: इसका अधिकेंद्र मांडले (म्यांमार का दूसरा सबसे बड़ा शहर है), म्यांमार से 17.2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित था।
- प्रभावित क्षेत्र:
- यह भूकंप म्यांमार के प्रमुख शहर मंडाले (Mandalay) और राजधानी नेप्यीदा (Nay Pyi Taw) के करीब था।
- इसमें मंडाले, सागाइंग, बागो, मैगवे, शान और नेप्यीदा सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र रहे।
- इस भूकंप का असर थाईलैंड, भारत, बांग्लादेश और दक्षिण-पश्चिम चीन तक महसूस किया गया।
- प्रभाव:
- सरकारी आंकड़ों के अनुसार मृतकों की संख्या 2,700 से अधिक है।
- 441 से अधिक लोग इस विनाशकारी भूकंप में लापता हो गए है।
- म्यांमार में आए शक्तिशाली भूकंप से देश के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का लगभग 70% तक नुकसान हुआ है।
- इसमें 1,500 से अधिक इमारतें, कई पुल और सड़कें क्षतिग्रस्त हुई है।
- मानवीय सहायता:
- थाईलैंड, चीन, भारत, रूस और संयुक्त राष्ट्र ने म्यांमार को आपातकालीन सहायता देने की घोषणा की।
- इसमें संयुक्त राष्ट्र और रेड क्रॉस ने $100 मिलियन की सहायता राशि जमा करने की अपील की।
- इसके लिए भारत ने ‘ऑपरेशन ब्रह्मा’ शुरू किया। इसके तहत: 15 टन राहत सामग्री व 80 सदस्यों वाली NDRF टीम भेजी गई। साथ ही INS सतपुड़ा व INS सावित्री ने 40 टन मानवीय सहायता यांगून पहुंचाई।
- म्यांमार में अब तक आए भूकंप:
- 1839 का सबसे भीषण भूकंप – यह म्यांमार का अब तक का सबसे शक्तिशाली भूकंप था, जिसकी तीव्रता 8.3 थी और इसमें अनुमानित 300-400 लोग मारे गए थे।
- जनवरी 1990 का भूकंप – 7.0 तीव्रता वाले इस भूकंप में 32 से अधिक इमारतें क्षतिग्रस्त हो गईं।
- 2016 का भूकंप – अगस्त 2016 में आए 6.8 तीव्रता के भूकंप से सैकड़ों ऐतिहासिक बौद्ध स्तूपों और मंदिरों को नुकसान पहुंचा।
म्यांमार में इस तरह के भूकंप आने के प्रमुख कारण
- भूगर्भीय संरचना: म्यांमार चार प्रमुख टेक्टोनिक प्लेटों – यूरेशियन, भारतीय, सुंडा और बर्मा प्लेट के अभिसरण बिंदु पर स्थित है। इन प्लेटों की आपसी टक्कर और निरंतर गति के कारण यह क्षेत्र विश्व के सबसे अधिक भूकंप-प्रवण क्षेत्रों में गिना जाता है। टेक्टोनिक गतिविधियों की तीव्रता के कारण यहां बार-बार शक्तिशाली भूकंप आते रहते हैं।
- टेक्टोनिक प्लेटों की परस्पर गति: म्यांमार एक संवेदनशील भूकंपीय क्षेत्र में स्थित है, जहां भारतीय और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेटें आपस में टकराती हैं। भारतीय प्लेट उत्तर की ओर गति कर रही है, जिससे यूरेशियन प्लेट के साथ घर्षण बढ़ता है। यह परस्पर गति तनाव उत्पन्न करती है, और जब यह तनाव अचानक मुक्त होता है, तो तेज भूकंपीय ऊर्जा बाहर निकलती है, जिससे भूकंप आता है।
- सागाइंग भ्रंश की सक्रियता: सागाइंग भ्रंश (Sagaing Fault) म्यांमार का सबसे लंबा और सक्रिय भ्रंश है, जो देश के मध्य भाग में उत्तर-दक्षिण दिशा में फैला हुआ है। यह भ्रंश 1,500 किमी लंबा है और पश्चिम में भारतीय प्लेट तथा पूर्व में यूरेशियन प्लेट को विभाजित करता है। ‘स्ट्राइक-स्लिप फॉल्टिंग’ के कारण यहां अक्सर भूकंप आते हैं, जिसमें चट्टानें क्षैतिज दिशा में एक-दूसरे के सापेक्ष खिसकती हैं।
- भूकंपीय उथल-पुथल: म्यांमार के इस क्षेत्र में लगातार टेक्टोनिक तनाव जमा होता रहता है, क्योंकि यह दुनिया के सबसे सक्रिय भूकंपीय क्षेत्रों में से एक है। इस बार भी भूकंप से पहले फॉल्ट लाइन के किनारे भारी दबाव बढ़ गया था, जो अंततः 7.7 तीव्रता के शक्तिशाली झटके के रूप में बाहर आया। कम गहराई (10 किमी) पर केंद्रित होने के कारण इसका असर तेजी से और व्यापक रूप से महसूस हुआ।
भूकंप से संबंधित जानकारी
|
भूकंप के आने में भ्रंश (Fault) की भूमिका
पृथ्वी की सतह के नीचे विशाल चट्टानी प्लेटों की हलचल भूकंप का प्रमुख कारण होती है। इस हलचल को नियंत्रित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण भूवैज्ञानिक तत्व भ्रंश (Fault) है।
- भ्रंश एक भूवैज्ञानिक दरार है, जो पृथ्वी की ऊपरी परत में चट्टानों को विभाजित करती है।
- यह दरारें या तो संकीर्ण हो सकती हैं या बड़े क्षेत्रों तक फैली हो सकती हैं।
- भ्रंश के दोनों ओर मौजूद चट्टानी ब्लॉक आपस में घर्षण (Friction) के कारण फंसे रहते हैं, लेकिन जब ऊर्जा अचानक मुक्त होती है, तो भूकंप आता है।
- भ्रंश को उनके झुकाव (Dip) और खिसकने की दिशा (Slip) के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है।
- निर्माण: भ्रंश का निर्माण तब होता है जब टेक्टोनिक प्लेटों में संचित तनाव (Tectonic Stress) एक सीमा से अधिक बढ़ जाता है और चट्टानें टूट जाती हैं।
- टूटने की यह प्रक्रिया वर्षों या सदियों में धीरे-धीरे होती रहती है, लेकिन जब अचानक ऊर्जा मुक्त होती है, तो यह भूकंप का कारण बनती है।
- भ्रंश के प्रकार:
- सामान्य भ्रंश (Normal Fault): इस भ्रंश में चट्टानी खंड एक-दूसरे से दूर हटते हैं, जिससे ऊपरी ब्लॉक नीचे की ओर खिसक जाता है। यह मुख्य रूप से तनाव (Tension) वाले क्षेत्रों में पाया जाता है, जहाँ चट्टानों पर खिंचाव बल लगता है।
- थ्रस्ट भ्रंश (Thrust Fault): इसमें ऊपरी चट्टानी ब्लॉक, निचले ब्लॉक पर चढ़ जाता है। यह संपीड़न (Compression) वाले क्षेत्रों में पाया जाता है, जहाँ चट्टानें एक-दूसरे की ओर धकेली जाती हैं। यह सबसे विनाशकारी भ्रंशों में से एक है।
- स्ट्राइक-स्लिप भ्रंश (Strike-Slip Fault): इसमें चट्टानी खंड क्षैतिज दिशा में एक-दूसरे के सापेक्ष विपरीत दिशाओं में खिसकते हैं। यह उन क्षेत्रों में होता है, जहाँ प्लेटों पर पार्श्व (Shear) बल लगता है। इसे दो प्रकारों में विभाजित किया जाता है:
- दाएँ-पार्श्व भ्रंश (Right-Lateral Fault) – जब सामने वाले ब्लॉक को देखने पर वह दाईं ओर खिसकता दिखाई दे।
- बाएँ-पार्श्व भ्रंश (Left-Lateral Fault) – जब सामने वाले ब्लॉक को देखने पर वह बाईं ओर खिसकता दिखाई दे।
विश्वभर में भूकंप के प्रमुख क्षेत्र
कुछ क्षेत्र विशेष रूप से भूकंप के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं, जिन्हें भूकंप बेल्ट (Earthquake Belts) कहा जाता है। ये बेल्ट पृथ्वी की उन दरारों (Fault Lines) और टेक्टोनिक सीमाओं (Tectonic Boundaries) के आसपास स्थित होते हैं, जहाँ प्लेटों की टकराहट और हलचल सबसे अधिक होती है।
- सर्कम-पैसिफिक बेल्ट: यह पृथ्वी का सबसे सक्रिय भूकंपीय क्षेत्र है, जिसे ‘रिंग ऑफ फायर’ के नाम से जाना जाता है। इस क्षेत्र में दुनिया के लगभग 81% भूकंप आते हैं। यह प्रशांत महासागर (Pacific Ocean) के चारों ओर फैला हुआ है, जिसमें जापान, इंडोनेशिया, फिलीपींस, न्यूज़ीलैंड, अमेरिका (कैलिफ़ोर्निया, अलास्का) और दक्षिण अमेरिका (चिली, पेरू) शामिल हैं।
- प्रमुख भूकंप: 2011 का जापान का भूकंप (9.0 तीव्रता), 1960 का चिली भूकंप (9.5 तीव्रता, अब तक का सबसे शक्तिशाली भूकंप)।
- एल्पाइड भूकंप बेल्ट: यह भूकंप क्षेत्र यूरोप और एशिया के पर्वतीय क्षेत्रों में फैला हुआ है, जिसमें हिमालय, ईरान, तुर्की, इटली और ग्रीस शामिल हैं। यहाँ पर दुनिया के लगभग 17% बड़े भूकंप आते हैं। यह क्षेत्र मुख्य रूप से भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट की टकराहट के कारण सक्रिय रहता है, जिससे हिमालय जैसे पर्वतों का निर्माण हुआ है।
- प्रमुख भूकंप: 2005 का कश्मीर भूकंप (7.6 तीव्रता), 2015 का नेपाल भूकंप (7.8 तीव्रता)।
- मिड-अटलांटिक रिज: यह क्षेत्र मुख्य रूप से अटलांटिक महासागर के तल में स्थित है, जहाँ पृथ्वी की क्रस्ट लगातार बन रही है और प्लेटें दूर खिसक रही हैं।
- यह एक डायवर्जेंट प्लेट सीमा (Divergent Plate Boundary) है, जहाँ दो टेक्टोनिक प्लेटें विपरीत दिशाओं में खिसक रही हैं, जिससे समुद्र तल पर दरारें बन रही हैं।
- हालाँकि यह क्षेत्र अधिकतर महासागर के अंदर स्थित है, लेकिन कभी-कभी इसकी गतिविधियाँ आइसलैंड और अटलांटिक द्वीपों पर महसूस की जाती हैं।
भारत में भूकंप और विभिन्न सिस्मिक जोन
भारत भौगोलिक रूप से एक भूकंप संभावित क्षेत्र है, जहाँ विभिन्न क्षेत्रों को उनके भूकंपीय (Seismic) गतिविधियों के आधार पर चार सिस्मिक जोन (Seismic Zones) में विभाजित किया गया है। नवंबर 2024 से फरवरी 2025 के बीच भारत में कुल 159 भूकंप दर्ज किए गए, जिससे देश में भूकंपीय गतिविधि बढ़ने का संकेत मिलता है।
- सिस्मिक जोन II – यह क्षेत्र भूकंप की दृष्टि से सबसे कम सक्रिय (Least Active) जोन है, जहाँ भूकंप आने की संभावना बहुत ही कम रहती है।
- भारत का लगभग 41% क्षेत्र इस जोन में आता है।
- यह क्षेत्र संरचनात्मक रूप से सबसे सुरक्षित माना जाता है, क्योंकि यहाँ भूकंप की तीव्रता और प्रभाव नगण्य होते हैं।
- सिस्मिक जोन III – इस क्षेत्र में भूकंप की संभावना मध्यम स्तर की होती है, यानी न तो बहुत अधिक और न ही बहुत कम।
- भारत के लगभग 30% हिस्से को यह जोन कवर करता है।
- यहाँ भूकंप से मध्यम स्तर का नुकसान हो सकता है, इसलिए भवन निर्माण के दौरान विशेष सावधानियाँ बरती जाती हैं।
- सिस्मिक जोन IV – यह क्षेत्र भूकंप की उच्च संभावना वाला क्षेत्र है, जहाँ ज़मीन में दरारें पड़ने, इमारतों के गिरने और अन्य गंभीर प्रभाव हो सकते हैं।
- भारत के कई बड़े शहर और पर्वतीय क्षेत्र इस जोन में आते हैं, जहाँ भूकंपीय गतिविधियाँ अधिक होती हैं।
- इन क्षेत्रों में भूकंपरोधी निर्माण तकनीकों का इस्तेमाल अनिवार्य होता है।
- सिस्मिक जोन V – इस जोन में सबसे तीव्र और विनाशकारी भूकंप आने की संभावना रहती है।
- भारत के लगभग 11% हिस्से को यह जोन कवर करता है, जिसमें हिमालयी क्षेत्र, उत्तर-पूर्वी भारत और कुछ अन्य संवेदनशील राज्य आते हैं।
- यहाँ भूकंप से सबसे अधिक जान-माल का नुकसान होने की संभावना होती है, इसलिए यह क्षेत्र अत्यधिक जोखिम (High Risk Zone) का हिस्सा माना जाता है।
भारत में अब तक आए विनाशकारी भूकंप
- 1905 का कांगड़ा भूकंप – हिमाचल प्रदेश में 4 अप्रैल 1905 को आए कांगड़ा भूकंप ने भारतीय उपमहाद्वीप को झकझोर कर रख दिया। 8.0 की तीव्रता वाले इस भूकंप में लगभग 19,800 लोगों की जान चली गई और हजारों मकान पूरी तरह नष्ट हो गए। यह भूकंप इतना शक्तिशाली था कि इसकी गूंज दिल्ली तक महसूस की गई थी। कांगड़ा और उसके आसपास के इलाके इस भूकंप से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए थे।
- 2001 का भुज भूकंप – 26 जनवरी 2001, जब पूरा देश गणतंत्र दिवस मना रहा था, उसी समय गुजरात के भुज शहर में 7.9 तीव्रता का भूकंप आया, जिसने पूरे राज्य में तबाही मचा दी। इस भूकंप में 12,932 लोगों की मौत हुई और लाखों लोग बेघर हो गए। भुज और आसपास के क्षेत्रों में सड़कों, इमारतों और बुनियादी ढांचे को भारी क्षति पहुंची। यह भारत के इतिहास में सबसे विनाशकारी भूकंपों में से एक था।
- 2025 दिल्ली भूकंप – हाल ही में 17 फरवरी 2025 को दिल्ली में 4.0 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया, जिससे हल्के झटके महसूस किए गए। हालांकि, कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन यह भूकंप संकेत देता है कि दिल्ली और आसपास के क्षेत्र भूकंपीय रूप से संवेदनशील हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि दिल्ली-एनसीआर जोन IV में आता है, जहां भविष्य में अधिक तीव्रता वाले भूकंप आ सकते हैं।
भारत में भूकंप सुरक्षा के लिए सरकारी पहल
- भूकंप विज्ञान केंद्रों में वृद्धि: भारत सरकार ने भूकंप निगरानी नेटवर्क को मजबूत करने के लिए सिस्मिक वेधशालाओं की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि की है। 2014 में जहां केवल 80 सिस्मिक वेधशालाएँ थीं, वहीं फरवरी 2025 तक इनकी संख्या 168 हो गई। यह पहल भूकंप गतिविधियों की वास्तविक समय में निगरानी और सटीक पूर्वानुमान लगाने में मदद कर रही है।
- 10-सूत्रीय एजेंडा: 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए 10-सूत्रीय एजेंडा प्रस्तुत किया था, जो विजन डॉक्यूमेंट 2047 के तहत एक आपदा-लचीला भारत बनाने की दिशा में कार्य कर रहा है।
- भूकंप-रोधी निर्माण: भारत का लगभग 59% भू-भाग भूकंप संभावित क्षेत्र में आता है, जिसके कारण भवन संहिता (Building Code) को सख्ती से लागू किया जा रहा है। सरकारी योजनाओं के तहत पुरानी इमारतों को भूकंप-रोधी बनाने के लिए रेट्रोफिटिंग (Retrofitting) की प्रक्रिया अपनाई जा रही है।
- सरल दिशा-निर्देश: सरकार ने 2021 में भूकंप सुरक्षा दिशा-निर्देशों को सरल बनाकर प्रभावी बनाया। भवन संहिता में किए गए सुधारों के तहत नई इमारतों और अपार्टमेंट में भूकंप सुरक्षा मानकों का पालन अनिवार्य किया गया है।
- “भूकंप ऐप”: राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र (NCS) द्वारा “भूकंप” (Bhookamp) नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। यह रियल-टाइम भूकंप की जानकारी प्रदान करता है और लोगों को सुरक्षित रहने के लिए सतर्क करता है।
- राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र (NCS): भारत में भूकंप निगरानी का कार्य राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र (NCS) द्वारा किया जाता है, जिसकी शुरुआत 1898 में कोलकाता (अलीपुर) में पहली भूकंपीय वेधशाला से हुई थी। आज देशभर में उन्नत भूकंपीय नेटवर्क स्थापित किया गया है, जिससे भूकंप गतिविधियों की लगातार निगरानी की जाती है।
- भूकंप जोखिम इंडेक्सिंग (EDRI): राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) ने भूकंप जोखिम इंडेक्सिंग (Earthquake Disaster Risk Index – EDRI) परियोजना शुरू की है। इसका उद्देश्य भारतीय शहरों में भूकंप के जोखिमों का वैज्ञानिक रूप से मूल्यांकन करना है। इस परियोजना के पहले चरण में 50 शहरों को शामिल किया गया और दूसरे चरण में 16 और शहरों को जोड़ा गया।
UPSC पिछले वर्षों के प्रश्न (PYQs) प्रश्न (2015): भारतीय उपमहाद्वीप में भूकंप की आवृत्ति में वृद्धि हुई है। हालांकि, उनके प्रभाव को कम करने के लिए भारत की तैयारियों में महत्वपूर्ण खामियां हैं। विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करें। प्रश्न (2021): भूकंप संबंधी खतरों के प्रति भारत की संवेदनशीलता के बारे में चर्चा करें। पिछले तीन दशकों के दौरान भारत के विभिन्न भागों में भूकंप के कारण हुई प्रमुख आपदाओं की मुख्य विशेषताओं सहित उदाहरण दें। |
Explore our Books: https://apnipathshala.com/product-category/books/
Explore Our test Series: https://tests.apnipathshala.com/