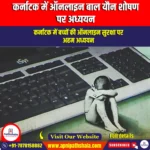सामान्य अध्ययन पेपर II: संवैधानिक निकाय, पारदर्शिता और जवाबदेहिता |
चर्चा में क्यों?
ज्ञानेश कुमार को 17 फरवरी 2025 को भारत का नया मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। वह वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार की जगह लेंगे। इस नियुक्ति से चुनाव आयोग के संचालन और निर्वाचन प्रक्रिया में नए दृष्टिकोण की संभावना बनी है।
भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से संबंधित जानकारी
भारत के चुनाव आयोग में एक महत्वपूर्ण बदलाव हुआ है। इसके तहत ज्ञानेश कुमार को 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त (Chief Election Commissioner- CEC) के रूप में नियुक्त किया गया है।
- जन्म: 27 जनवरी 1964
- शिक्षा:
- B.Tech (सिविल इंजीनियरिंग) – IIT कानपुर
- ICFAI से बिजनेस फाइनेंस
- हार्वर्ड विश्वविद्यालय (HIID) से पर्यावरण अर्थशास्त्र
- IAS कैडर: 1988 बैच के केरल कैडर के अधिकारी
- कार्यकाल: ज्ञानेश कुमार का कार्यकाल 26 जनवरी 2029 तक रहेगा। इस दौरान वे कई महत्वपूर्ण चुनावों की जिम्मेदारी निभाएंगे, जिनमें:
- बिहार विधानसभा चुनाव (2025)
- केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु, और पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव (2026)
- अनुभव:
- केरल सरकार में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर कार्य (जैसे सहायक जिलाधिकारी, उपजिलाधिकारी, SC/ST डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के MD)
- भारत सरकार में रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, और संसदीय कार्य मंत्रालय में महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया
- गृह मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव के रूप में जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निरस्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
- राम मंदिर के सुप्रीम कोर्ट के मामले से संबंधित दस्तावेजों को संभाला।
- केरल से लेकर भारत सरकार तक विभिन्न क्षेत्रों में काम किया, जिसमें फास्ट-ट्रैक परियोजनाएं, वित्त संसाधन और लोक निर्माण विभाग जैसे विभाग शामिल हैं।
मुख्य चुनाव आयुक्त कौन होते हैं?
मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) भारतीय चुनाव आयोग का सर्वोच्च अधिकारी होता है और भारतीय लोकतंत्र में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मुख्य चुनाव आयुक्त, चुनाव आयोग का नेतृत्व करता है और निर्वाचन प्रक्रिया को स्वतंत्र, निष्पक्ष, और पारदर्शी बनाने की जिम्मेदारी निभाता है। यह पद भारतीय लोकतंत्र के महत्वपूर्ण संवैधानिक पदों में से एक माना जाता है।
- नियुक्ति प्रक्रिया:
- नवीन अधिनियम: 2023 में लागू किए गए “नियुक्ति, सेवा शर्तें और कार्यकाल अधिनियम” के तहत मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति प्रक्रिया में बदलाव आया है। अब यह चयन एक तीन सदस्यीय समिति द्वारा किया जाता है, जिसमें प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और एक केंद्रीय मंत्री होते हैं।
- सिफारिश और चयन: इस चयन समिति से पहले एक खोज समिति पांच संभावित उम्मीदवारों के नाम सुझाती है, जिनमें से एक नाम को चयन समिति द्वारा अंतिम रूप से चुना जाता है। फिर इस नाम को राष्ट्रपति को भेजा जाता है और राष्ट्रपति द्वारा अंतिम मंजूरी मिलने के बाद नियुक्ति का नोटिफिकेशन जारी किया जाता है।
- पूर्व प्रक्रिया: इससे पहले, नियुक्तियां प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती थीं, जो अब नई प्रक्रिया में बदल गई है।
- कार्यकाल और अधिकार
- कार्यकाल: मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है, जो पहले हो।
- अधिकार: CEC को चुनाव कार्यक्रम तय करने, आचार संहिता लागू करने और चुनाव रद्द करने की शक्ति प्राप्त होती है यदि किसी गड़बड़ी या अनियमितता का पता चलता है। इसके अलावा, वे चुनावी प्रक्रिया से संबंधित निर्देश भी जारी कर सकते हैं।
- योग्यता: मुख्य चुनाव आयुक्त बनने के लिए उम्मीदवार को भारत सरकार के सचिव-स्तर का अधिकारी होना चाहिए, जो इस पद की उच्चतम जिम्मेदारी निभा सके।
- कर्तव्य
- मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्य लोकसभा, राज्य विधानसभा, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनावों का संचालन करना है। इसके अलावा, उन्हें निम्नलिखित जिम्मेदारियाँ निभानी होती हैं:
- आचार संहिता का पालन: चुनावों के दौरान आचार संहिता का सख्ती से पालन सुनिश्चित करना।
- नए राजनीतिक दलों का पंजीकरण: नए राजनीतिक दलों को पंजीकरण और मान्यता देना।
- मतदान प्रतिशत बढ़ाना: चुनावों में अधिक से अधिक मतदान सुनिश्चित करने के लिए जागरूकता अभियान चलाना।
- चुनावी सुधार: लोकतंत्र को मज़बूत करने के लिए चुनावी प्रक्रियाओं में सुधार की सिफारिश करना।
- मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्य लोकसभा, राज्य विधानसभा, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनावों का संचालन करना है। इसके अलावा, उन्हें निम्नलिखित जिम्मेदारियाँ निभानी होती हैं:
- वेतन: मुख्य चुनाव आयुक्त का वेतन और सेवा शर्तें भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान होती हैं। इसका मतलब यह है कि उनका वेतन, भत्ते और अन्य लाभ सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बराबर होते हैं, जो उनके पद की गंभीरता और जिम्मेदारी को दर्शाता है।
- निष्कासन की प्रक्रिया
- मुख्य चुनाव आयुक्त को केवल महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा ही हटाया जा सकता है, जो संसद के माध्यम से होती है। यह प्रक्रिया उनके स्वतंत्रता को सुनिश्चित करती है।
- वे अपनी इच्छा से इस्तीफा दे सकते हैं या कार्यकाल की समाप्ति से पहले हटाए जा सकते हैं।
- सीमाएँ
- संविधान ने निर्वाचन आयुक्त के लिए किसी विशेष कानूनी, शैक्षिक, प्रशासनिक या न्यायिक योग्यता की आवश्यकता नहीं निर्धारित की है।
- संविधान में चुनाव आयोग के सदस्यों के कार्यकाल को लेकर कोई विशेष प्रावधान नहीं किया गया है।
भारत का चुनाव आयोग (ECI)
भारत का चुनाव आयोग (ECI) देश के चुनावी तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, जिसे भारतीय संविधान के तहत स्वायत्तता और अधिकार प्राप्त हैं। यह आयोग न केवल राष्ट्रीय चुनावों का आयोजन करता है, बल्कि संविधान में निर्दिष्ट प्रक्रियाओं के आधार पर चुनावों को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने की जिम्मेदारी भी निभाता है।
- चुनाव आयोग की स्थापना
- भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी। इस दिन को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है।
- चुनाव आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है।
- संविधान में चुनाव आयोग
- भारतीय संविधान का भाग XV (अनुच्छेद 324-329) चुनाव आयोग से संबंधित है, जिसमें आयोग की शक्तियां, कार्य और नियंत्रण की व्यवस्था की गई है।
- 324: चुनाव आयोग को चुनावों के सम्पूर्ण अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का दायित्व सौंपा गया है।
- 325: किसी भी व्यक्ति को धर्म, जाति या लिंग के आधार पर मतदाता सूची से बाहर रखने या मतदान के अधिकार से वंचित करने का प्रावधान नहीं है।
- 326: लोकसभा और प्रत्येक राज्य विधानसभा के चुनाव में वयस्क मताधिकार के आधार पर मतदान होगा।
- 327: चुनाव संबंधी कानून बनाने की शक्ति संसद को प्राप्त है।
- 328: किसी राज्य के विधानमंडल को राज्य चुनावों के लिए कानून बनाने की शक्ति है।
- 329: चुनावी मामलों में न्यायालयों द्वारा हस्तक्षेप पर रोक लगाई गई है।
- चुनाव आयोग की संरचना
- पहले, निर्वाचन आयोग में केवल एक चुनाव आयुक्त का प्रावधान था, लेकिन 16 अक्टूबर, 1989 से इसे तीन सदस्यीय आयोग बना दिया गया।
- वर्तमान में इसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) और दो अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं।
- राज्य स्तर पर निर्वाचन आयोग के कार्यों में सहायता मुख्य चुनाव अधिकारी (जो आईएएस अधिकारी होते हैं) द्वारा की जाती है।
चुनाव आयोग के कार्य और शक्तियाँ
- चुनाव आयोग का मुख्य कार्य चुनाव कार्यक्रम तय करना और पूरे चुनावी प्रक्रिया का संचालन करना है।
- यह समय-समय पर आम चुनाव और उप-चुनाव के कार्यक्रम तय करता है, ताकि निर्वाचन प्रक्रिया सही समय पर पूरी हो सके।
- आयोग निर्वाचक नामावली तैयार करता है, जिसमें सभी योग्य मतदाताओं का विवरण होता है।
- इसके साथ ही, मतदाता पहचान पत्र (EPIC) जारी करता है।
- आयोग मतदान और मतगणना केंद्रों के लिए स्थानों का चयन करता है।
- इन केंद्रों में आवश्यक व्यवस्थाएँ (जैसे सुरक्षा, मतदान की सुविधा आदि) और सुविधाओं का प्रबंध भी चुनाव आयोग करता है ताकि मतदान प्रक्रिया सही ढंग से चले।
- चुनाव आयोग राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करता है और उन्हें चुनाव चिह्न आवंटित करता है। इसके साथ ही, राजनीतिक दलों से संबंधित विवादों का निपटारा भी चुनाव आयोग करता है।
- आयोग आदर्श आचार संहिता जारी करता है, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि चुनाव के दौरान कोई भी पार्टी या उम्मीदवार अनुचित कार्य न करें या सत्ता का दुरुपयोग न हो।
- आयोग प्रत्येक उम्मीदवार के चुनाव अभियान खर्च की सीमा तय करता है और उसकी निगरानी भी करता है।
- यदि संसद या राज्य विधानसभाओं के सदस्य चुनाव नियमों का उल्लंघन करते हैं, तो आयोग उन्हें अयोग्य ठहरा सकता है।
- आयोग को निर्वाचन क्षेत्र की सीमाओं का निर्धारण करने का अधिकार प्राप्त है।
- आयोग को यह अधिकार है कि यदि चुनावी प्रक्रिया में गड़बड़ी या अनियमितता पाई जाती है, तो वह चुनाव रद्द कर सकता है।
- इसके अलावा, आयोग चुनावी भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों पर राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी राय भी प्रस्तुत करता है।
निर्वाचन आयोग के समक्ष प्रमुख चुनौतियाँ
भारत का निर्वाचन आयोग (ECI) लोकतंत्र की नींव है, जो चुनावों की स्वतंत्रता और निष्पक्षता सुनिश्चित करता है। हालांकि, आयोग को विभिन्न चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जो उसकी प्रभावशीलता और निष्पक्षता पर सवाल उठाती हैं।
- राजनीति का अपराधीकरण: भारतीय राजनीति में वर्षों से हिंसा, चुनावी दुर्भावनाएँ और काले धन का बोलबाला बढ़ा है, जिससे राजनीति का अपराधीकरण हुआ है। निर्वाचन आयोग के लिए इस आपराधिक तत्त्वों और काले धन के प्रभाव को नियंत्रित करना एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि यह लोकतांत्रिक प्रक्रिया को प्रभावित करता है।
- आचार संहिता का उल्लंघन: चुनावों के दौरान सरकारी वाहनों और सरकारी भवनों का इस्तेमाल आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के रूप में किया जाता है। चुनावों के दौरान राज्य सरकारों द्वारा सत्ता का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग किया जाता है। आयोग के लिए यह एक कठिन चुनौती है, क्योंकि यह चुनावों की निष्पक्षता को प्रभावित करता है, और इसे रोकने के लिए अधिक प्रभावी उपायों की आवश्यकता है।
- निष्पक्षता: राजनीतिक दलों के आंतरिक लोकतंत्र और उनके वित्तीय विनियमन को सुनिश्चित करने की भी कोई कानूनी शक्ति आयोग के पास नहीं है, जिससे चुनावों में पारदर्शिता बनाए रखना मुश्किल हो जाता है। ईवीएम में खराबी, हैकिंग और वोट दर्ज न होने के आरोपों ने आम जनता के बीच निर्वाचन आयोग के प्रति विश्वास को कम किया है। नैतिकता सुनिश्चित करने के लिए यह आवश्यक है कि आयोग में कुशल और योग्य व्यक्ति उच्च पदों पर नियुक्त हों।
UPSC पिछले वर्षों के प्रश्न (PYQs) प्रश्न (2017): निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं ? (a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 (c) केवल 2 और 3 (d) केवल 3 उत्तर: (d) प्रश्न (2022): आदर्श आचार-संहिता के उद्भव के आलोक में, भारत के निर्वाचन आयोग की भूमिका का विवेचन कीजिये। |
Explore our Books: https://apnipathshala.com/product-category/books/
Explore Our test Series: https://tests.apnipathshala.com/