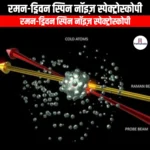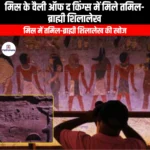Kolhan Manki-Munda System
संदर्भ:
झारखंड के पश्चिम सिंहभूम जिले में हो जनजाति के आदिवासियों ने पारंपरिक आत्म-शासन प्रणाली ‘मानकी-मुंडा’ में हस्तक्षेप के आरोप लगाते हुए उपायुक्त (DC) के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया।
मांकी–मुंडा व्यवस्था:
पारंपरिक शासन व्यवस्था:
- मांकी-मुंडा प्रणाली झारखंड के कोल्हान क्षेत्र में हो जनजाति की पारंपरिक स्वशासन प्रणाली है।
- यह एक विकेन्द्रीकृत ढांचा है, जो सदियों से अस्तित्व में है और आज भी राज्य की औपचारिक प्रशासनिक प्रणाली के साथ समानांतर रूप से कार्य करता है।
संरचना:
- मुंडा (ग्राम प्रधान): वंशानुगत ग्राम प्रमुख, जो गाँव के सामाजिक और राजनीतिक विवादों का निपटारा करते हैं।
- मांकी (मुखिया): 8–15 गाँवों के समूह (पीर) का नेतृत्व करता है और वे मामले देखता है जिन्हें मुंडा सुलझा नहीं पाते।
- प्रारंभ में मांकी और मुंडा का भूमि या राजस्व संबंधी कार्यों से कोई सरोकार नहीं था।
ब्रिटिश हस्तक्षेप:
- स्थायी बंदोबस्त अधिनियम (1793): जमींदारों ने हो जनजाति की भूमि हड़पनी शुरू की, जिससे हो विद्रोह (1821–22) और कोल विद्रोह (1831–32) जैसे आंदोलन हुए।
- विल्किंसन नियम (1833):
- ब्रिटिश अधिकारी कैप्टन थॉमस विल्किंसन ने मांकी-मुंडा व्यवस्था को 31 नियमों में संहिताबद्ध किया।
- मांकी और मुंडा को सामुदायिक नेता तो माना गया, पर उन्हें औपनिवेशिक प्रशासन का एजेंट बना दिया गया।
- इसके जरिए कोल्हान क्षेत्र ब्रिटिश भारत में शामिल हुआ, निजी संपत्ति, पट्टे और गैर-आदिवासी (दिक्कुओं) का प्रवेश शुरू हुआ।
- हो लोगों को रैयत (किरायेदार) घोषित किया गया।
स्वतंत्रता के बाद:
- 1947 के बाद कोल्हान गवर्नमेंट एस्टेट समाप्त कर दिया गया, लेकिन विल्किंसन नियम को भारतीय न्यायालयों ने रिवाज (Custom) के रूप में मान्यता दी।
- 2021 में झारखंड सरकार ने पारंपरिक न्याय प्रणाली न्याय पंचायत को मान्यता दी, जिसे राजस्व कार्य, कर संग्रह, भूमि लेन-देन, कानून-व्यवस्था और विवाद निपटान जैसे कार्य भी सौंपे गए।
मांकी–मुंडा प्रणाली की समस्याएँ
- वंशानुगत उत्तराधिकार:
- मांकी और मुंडा के पद प्रायः पिता से पुत्र को मिलते हैं।
- इससे योग्य व्यक्तियों को नेतृत्व के अवसर नहीं मिल पाते।
- औपचारिक शिक्षा का अभाव: कई पारंपरिक नेता निरक्षर हैं और उन्हें भूमि अभिलेख, दस्तावेज़ प्रबंधन तथा आधुनिक प्रशासनिक कार्यों का प्रशिक्षण नहीं है।
- अनुपस्थित नेतृत्व: कई बार मुंडा लंबे समय तक गाँव से बाहर रहते हैं, जिससे ग्रामीणों को बुनियादी सेवाओं तक पहुँच नहीं मिल पाती।
- गैर–आदिवासी समुदायों के साथ तनाव: अनुसूचित जाति (SC) और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) जैसे गैर-आदिवासी समूहों ने भेदभाव और आजीविका पर प्रतिबंध की शिकायत की है।
- रिक्त पद: पश्चिम सिंहभूम में लगभग 1,850 स्वीकृत पदों में से करीब 200 पद खाली हैं, जिससे जमीनी स्तर पर शासन प्रभावित होता है।
- नियमों की सीमित समझ: अधिकांश नेता विल्किंसन नियम (1833) या 1837 के हुक़ूकनामा को पूरी तरह नहीं समझते, जिससे विवाद निपटान जटिल हो जाता है।
- राज्य अधिकारियों पर निर्भरता: कई बार ग्रामीण सीधे उपायुक्त (Deputy Commissioner) से संपर्क करते हैं, जिससे मांकी-मुंडा प्रणाली की प्रभावशीलता और अधिकारिता कम हो जाती है।
- सुधार की मांग: हो समुदाय का एक वर्ग, विशेषकर युवा पीढ़ी, मांकी-मुंडा प्रणाली में सुधार चाहता है।