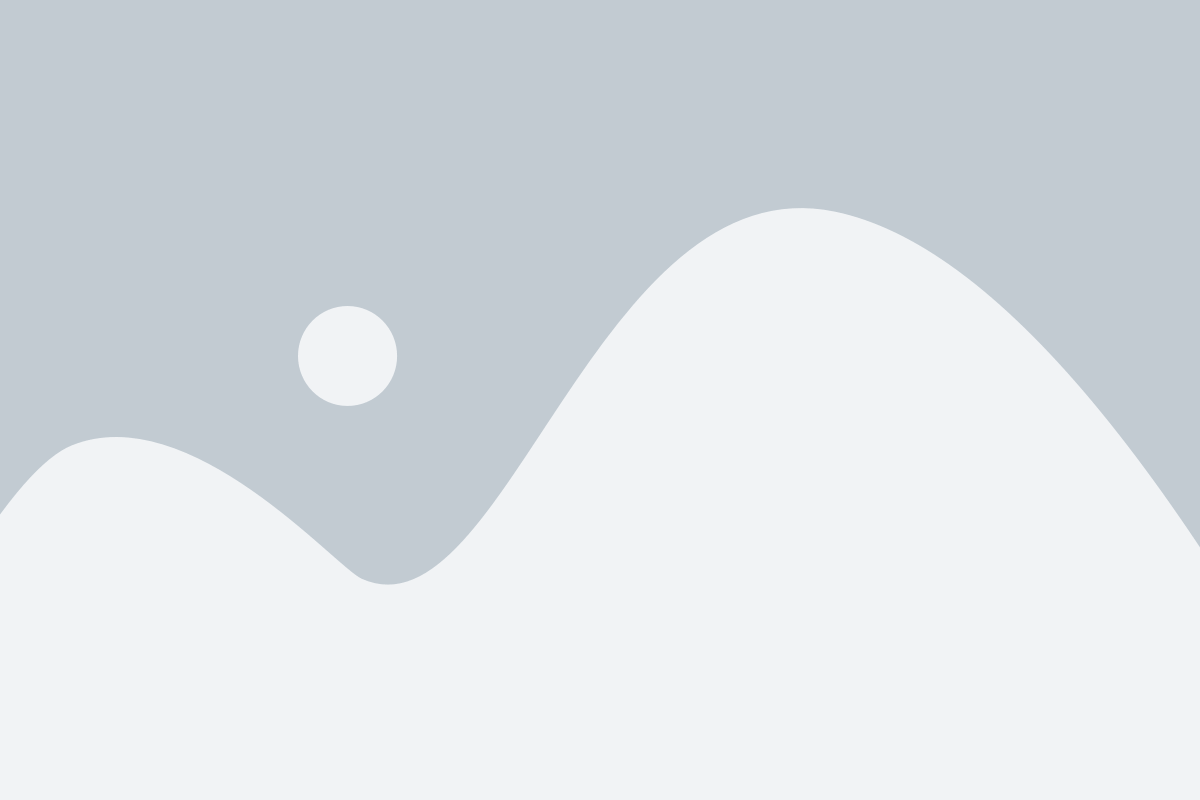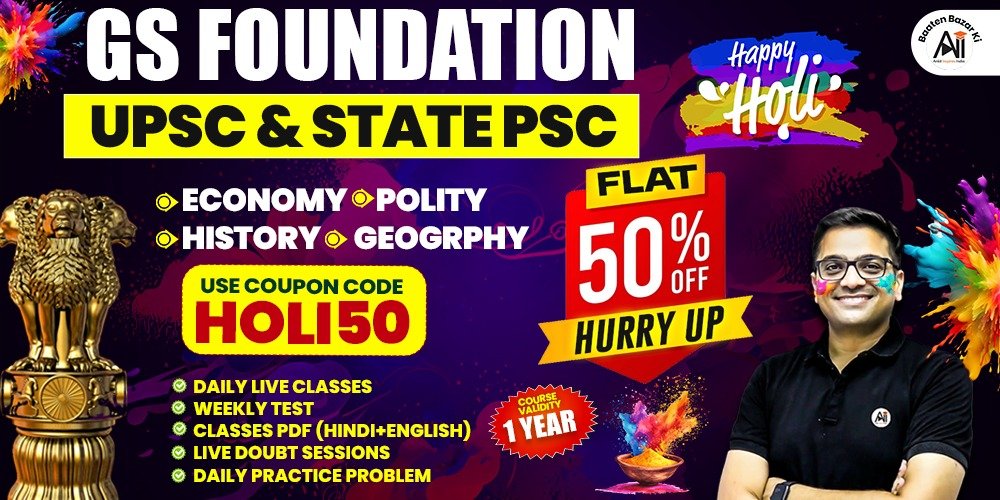|
सामान्य अध्ययन पेपर II: गवर्नर की भूमिका, केंद्र-राज्य संबंध, आपातकालीन प्रावधान |
चर्चा में क्यों?
हाल ही में मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह के इस्तीफे के बाद 11वीं बार मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया। राज्य में लंबे समय से जारी हिंसा, प्रशासनिक अस्थिरता और कानून-व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति के कारण यह निर्णय लिया गया।
राष्ट्रपति शासन की अवधारणा
राष्ट्रपति शासन एक ऐसी स्थिति है जिसमें राज्य सरकार को भंग करके केंद्र सरकार सीधे उस राज्य का शासन अपने हाथ में ले लेती है। यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत किया जाता है।
- राष्ट्रपति शासन तब लगाया जाता है जब राज्यपाल को लगता है कि राज्य सरकार संविधान के अनुसार काम नहीं कर रही है या राज्य में संवैधानिक संकट पैदा हो गया है। राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रपति यह फैसला लेते हैं कि राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाना है या नहीं। इसे ‘राज्य आपातकाल’ या ‘संवैधानिक आपातकाल’ के रूप में भी जाना जाता है।
- राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए राष्ट्रपति एक उद्घोषणा जारी करते हैं। इस उद्घोषणा में कहा जाता है कि राज्य सरकार को भंग कर दिया गया है और केंद्र सरकार अब राज्य का शासन चलाएगी।
- यह दर्शाता है कि अब केंद्र सरकार उस राज्य पर सीधे तौर पर नियंत्रण कर सकती है और उस दौरान नियुक्त राज्यपाल को संबंधित राज्य का संवैधानिक प्रमुख माना जाता है।
राष्ट्रपति शासन का संवैधानिक आधार
भारतीय संविधान में संघीय ढांचे को बनाए रखने और राज्यों की संवैधानिक व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। राष्ट्रपति शासन का आधार मुख्य रूप से संविधान के अनुच्छेद 355, 356, 357 और 365 में निहित है।
- अनुच्छेद 355: यह अनुच्छेद केंद्र सरकार को यह अधिकार देता है कि वह भारत के प्रत्येक राज्य की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा करे। इसके तहत केंद्र सरकार को यह सुनिश्चित करना होता है कि राज्यों में शासन संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार संचालित हो। यदि किसी राज्य में आंतरिक अशांति (Internal Disturbance) जैसी परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं, तो केंद्र सरकार आवश्यक हस्तक्षेप कर सकती है।
- अनुच्छेद 356: यह अनुच्छेद राष्ट्रपति को यह अधिकार देता है कि यदि उन्हें यह विश्वास हो जाए कि किसी राज्य की सरकार संविधान के अनुसार कार्य करने में असमर्थ हो गई है, तो वे उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकते हैं। इस अनुच्छेद के तहत, राष्ट्रपति राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद को बर्खास्त कर सकते हैं और राज्यपाल के माध्यम से राज्य का प्रशासन चला सकते हैं। इस स्थिति में, राज्य की विधानसभा को निलंबित (Suspended) या भंग (Dissolved) किया जा सकता है।
- अनुच्छेद 357: जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है, तो संसद को यह अधिकार मिल जाता है कि वह उस राज्य की विधायी शक्तियों का प्रयोग कर सके। यदि राज्य की विधान सभा भंग कर दी गई हो, तो संसद उस राज्य से जुड़े कानून बना सकती है और वित्तीय अधिकारों का प्रयोग कर सकती है। इसमें केंद्र सरकार को यह अधिकार प्राप्त है कि वह राज्यपाल के माध्यम से आवश्यक प्रशासनिक आदेश जारी कर सके।
- अनुच्छेद 365: यह अनुच्छेद स्पष्ट करता है कि यदि राज्य सरकार केंद्र सरकार के संवैधानिक निर्देशों का पालन करने में विफल रहती है, तो यह माना जाएगा कि राज्य की सरकार संविधान के अनुसार कार्य नहीं कर रही है। ऐसी स्थिति में, राष्ट्रपति को यह अधिकार मिल जाता है कि वह अनुच्छेद 356 के तहत उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दें। यह प्रावधान राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिए बाध्य करता है कि वह संघ के निर्देशों का पालन करे।
राष्ट्रपति शासन लागू करने के कारण
भारत में राष्ट्रपति शासन लागू करने के कई कारण हो सकते हैं, जिनमें से कुछ मुख्य कारण इस प्रकार हैं:
- संवैधानिक तंत्र की विफलता: जब किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है, तो राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। संवैधानिक तंत्र की विफलता तब होती है जब राज्य सरकार संविधान के अनुसार काम नहीं कर रही होती है या राज्य में कानून और व्यवस्था की स्थिति बिगड़ जाती है।
- राजनीतिक अस्थिरता: जब किसी राज्य में राजनीतिक अस्थिरता होती है, तो राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। राजनीतिक अस्थिरता तब होती है जब राज्य सरकार अल्पमत में होती है या जब राज्य में बार-बार सरकारें बदल रही होती हैं।
- यदि किसी राज्य में चुनाव के बाद किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है और राज्यपाल द्वारा निर्धारित समय के भीतर कोई भी दल सरकार बनाने में सक्षम नहीं होता है, तो राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है।
- यदि किसी राज्य में गठबंधन सरकार चल रही है और गठबंधन टूट जाता है, जिसके कारण मुख्यमंत्री को विधानसभा में बहुमत का समर्थन खोना पड़ता है, तो राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है।
- यदि विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव के कारण मुख्यमंत्री को बहुमत की कमी होती है, तो राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है।
- कानून-व्यवस्था की स्थिति: जब किसी राज्य में कानून और व्यवस्था की स्थिति बिगड़ जाती है, तो राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। कानून और व्यवस्था की स्थिति तब बिगड़ती है जब राज्य में अपराध बढ़ जाते हैं या जब राज्य में हिंसा और अराजकता फैल जाती है।
- प्राकृतिक आपदा: यदि किसी राज्य में प्राकृतिक आपदा, महामारी या युद्ध जैसी अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण चुनावों को स्थगित करना पड़ता है, तो राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है।
राष्ट्रपति शासन लागू करने की प्रक्रिया
राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए एक संवैधानिक प्रक्रिया का पालन किया जाता है, जो राज्यपाल की रिपोर्ट से शुरू होती है और संसद की स्वीकृति के साथ आगे बढ़ती है। यह प्रक्रिया निम्नलिखित चरणों में पूरी होती है:
- राज्यपाल की रिपोर्ट: जब किसी राज्य की सरकार संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार शासन करने में असमर्थ हो जाती है, तो राज्यपाल राष्ट्रपति को एक रिपोर्ट भेजते हैं, जिसमें बताया जाता है कि राज्य में संवैधानिक संकट उत्पन्न हो गया है। यह रिपोर्ट राज्य में राजनीतिक अस्थिरता, कानून-व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति या किसी अन्य संवैधानिक विफलता के आधार पर दी जाती है। हालांकि, राज्यपाल की रिपोर्ट राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए अनिवार्य नहीं है—राष्ट्रपति अन्य स्रोतों से भी जानकारी लेकर निर्णय ले सकते हैं।
- राष्ट्रपति की संतुष्टि: जब राष्ट्रपति इस बात से संतुष्ट हो जाते हैं कि राज्य में संविधान के अनुरूप शासन संभव नहीं है, तो वे अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू करने की घोषणा (Proclamation) जारी करते हैं। इस घोषणा के बाद, राज्य सरकार निलंबित या भंग कर दी जाती है और राज्य का प्रशासन राज्यपाल के माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा संचालित किया जाता है।
- संसदीय अनुमोदन: राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद, इसे दो महीने के भीतर संसद की मंजूरी प्राप्त करनी होती है। संसद के दोनों सदनों (लोकसभा और राज्यसभा) को साधारण बहुमत से इस निर्णय को मंजूरी देनी होती है। यदि संसद इसे मंजूरी दे देती है, तो राष्ट्रपति शासन छह महीने तक जारी रहता है।
राष्ट्रपति शासन की अवधि और समाप्ति
- राष्ट्रपति शासन की प्रारंभिक अवधि: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत लागू किया गया राष्ट्रपति शासन प्रारंभ में अधिकतम छह महीने तक लागू रहता है। यदि राज्य में संवैधानिक संकट बना रहता है, तो इसे हर छह महीने पर संसद की स्वीकृति से अधिकतम तीन वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है।
- एक वर्ष से अधिक विस्तार: 1978 के 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत, राष्ट्रपति शासन को एक वर्ष से अधिक बढ़ाने के लिए निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना आवश्यक है:
- चुनाव आयोग यह प्रमाणित करे कि संबंधित राज्य में विधानसभा चुनाव कराना संभव नहीं है। यदि चुनाव आयोग चुनाव कराने की स्थिति में असमर्थता व्यक्त करता है, तो राष्ट्रपति शासन को आगे बढ़ाने की अनुमति दी जा सकती है।
- यदि राज्य के पूरे क्षेत्र या उसके किसी हिस्से में राष्ट्रीय आपातकाल (अनुच्छेद 352) लागू हो तो राष्ट्रपति शासन एक वर्ष से अधिक बढ़ सकता है। यदि राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त हो जाता है और चुनाव आयोग चुनाव कराने के लिए तैयार होता है, तो राष्ट्रपति शासन तीन वर्ष की अवधि पूरी होने से पहले भी समाप्त किया जा सकता है।
- राष्ट्रपति शासन की समाप्ति: राष्ट्रपति किसी भी समय अपनी नई उद्घोषणा जारी कर राष्ट्रपति शासन समाप्त कर सकते हैं। इस नई उद्घोषणा के लिए संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती। जैसे ही राज्य में नयी सरकार का गठन होता है, राष्ट्रपति शासन स्वतः समाप्त हो जाता है।
राष्ट्रपति शासन के दौरान प्रशासनिक व्यवस्था
राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद, राज्य की सामान्य लोकतांत्रिक प्रणाली निलंबित हो जाती है, और केंद्र सरकार के प्रत्यक्ष नियंत्रण में प्रशासनिक कार्य किए जाते हैं। इस दौरान विभिन्न प्रशासनिक संस्थाओं की भूमिका निम्नलिखित होती है:
- राज्यपाल की भूमिका: राज्यपाल राज्य का कार्यकारी प्रमुख बन जाता है और राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। राज्यपाल सभी प्रशासनिक और विधायी कार्यों का नियंत्रण अपने हाथ में लेता है और मुख्यमंत्री व मंत्रिपरिषद की जगह पूरी शासन व्यवस्था की देखरेख करता है। प्रशासनिक निर्णय लेने के लिए राज्यपाल नौकरशाहों (अधिकारियों) और केंद्र सरकार के निर्देशों पर निर्भर करता है।
- विधान सभा की स्थिति: राज्य की विधानसभा या तो निलंबित कर दी जाती है या भंग कर दी जाती है। निलंबन की स्थिति में विधानसभा का अस्तित्व बना रहता है, लेकिन वह किसी भी प्रकार का विधायी कार्य नहीं कर सकती। भंग होने की स्थिति में नए चुनाव होने तक विधानसभा समाप्त हो जाती है।
- संसद की भूमिका: संघीय संसद (लोकसभा और राज्यसभा) उस राज्य के विधायी कार्यों को नियंत्रित करती है। राष्ट्रपति शासन लागू होने के दौरान संसद को राज्य के प्रशासन के हर महत्वपूर्ण निर्णय की जानकारी दी जाती है।
- शासन पर प्रभाव: केंद्र सरकार और राज्यपाल द्वारा चलाया जाने वाला शासन पूरी तरह से नौकरशाही (ब्यूरोक्रेसी) पर निर्भर करता है। इस दौरान राज्य के किसी भी प्रकार के नए कानून पारित नहीं किए जाते। कई बार जनहितकारी और कल्याणकारी योजनाएं ठप पड़ जाती हैं क्योंकि नए निर्णय लेने में देरी होती है।
- लोकतांत्रिक प्रक्रिया: चुनाव आयोग छह महीने के भीतर चुनाव कराने के लिए जिम्मेदार होता है, ताकि लोकतांत्रिक शासन बहाल किया जा सके। यदि राज्य की परिस्थितियाँ चुनाव कराने के अनुकूल नहीं होतीं, तो संसद की मंजूरी से राष्ट्रपति शासन को और बढ़ाया जा सकता है। जैसे ही नया मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद चुने जाते हैं, राष्ट्रपति शासन स्वतः समाप्त हो जाता है।
राष्ट्रपति शासन से जुड़ा प्रमुख न्यायिक फैसला
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के दुरुपयोग को रोकने और केंद्र द्वारा राज्यों में मनमाने ढंग से राष्ट्रपति शासन लागू करने की प्रवृत्ति को नियंत्रित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कई ऐतिहासिक फैसले दिए हैं। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण फैसला एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघ (1994) का है, जिसने अनुच्छेद 356 की व्याख्या करते हुए इसकी सीमाएँ तय कीं।
- मामले की पृष्ठभूमि
- एस.आर. बोम्मई कर्नाटक में जनता दल सरकार के मुख्यमंत्री थे।
- 1989 में उनकी सरकार बर्खास्त कर दी गई और राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया।
- सरकार को विधानसभा में बहुमत साबित करने का अवसर नहीं दिया गया, जिससे यह फैसला मनमाना माना गया।
- सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप
- एस.आर. बोम्मई ने इस बर्खास्तगी को चुनौती दी और मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचा।
- 11 मार्च 1994 को 9-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने फैसला सुनाया कि यह संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन था।
- न्यायालय द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देश
- बहुमत परीक्षण सदन के पटल पर होना चाहिए, राज्यपाल या केंद्र सरकार के निर्देश से नहीं।
- राज्य सरकार को पहले स्पष्टीकरण देने का अवसर दिया जाना चाहिए।
- राष्ट्रपति की संतुष्टि पूर्णत: न्यायिक समीक्षा के अधीन होगी, अर्थात् इसे अदालत में चुनौती दी जा सकती है।
- राष्ट्रपति संसद को भंग नहीं कर सकता जब तक कि उसकी उद्घोषणा संसद द्वारा अनुमोदित न हो।
- सिर्फ प्रशासनिक विफलता राष्ट्रपति शासन लागू करने का कारण नहीं हो सकती, केवल संवैधानिक तंत्र की विफलता ही इसका आधार हो सकती है।
- केंद्र सरकार को अनुच्छेद 356 का प्रयोग संयम और विवेक से करना चाहिए, न कि राजनीतिक उद्देश्यों के लिए।
स्वतंत्र भारत में राष्ट्रपति शासन
स्वतंत्र भारत में 1950 से अब तक 29 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कुल 134 बार राष्ट्रपति शासन लागू किया जा चुका है। कभी संवैधानिक संकट, कभी राजनीतिक अस्थिरता, तो कभी कानून-व्यवस्था की विफलता के कारण केंद्र सरकार को अनुच्छेद 356 का प्रयोग करना पड़ा।
- जम्मू और कश्मीर (4,668 दिन – 12 वर्ष से अधिक): यह भारत का सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति शासन झेलने वाला राज्य रहा है। 1990 में आतंकवाद और अलगाववादी गतिविधियों के चलते राष्ट्रपति शासन लागू किया गया, जो बहुत लंबे समय तक जारी रहा।
- पंजाब (3,878 दिन – 10 वर्ष से अधिक): राज्य में आतंकवाद, हिंसा और कानून-व्यवस्था की गंभीर समस्या ने इस लंबी अवधि को जरूरी बना दिया।
- पुदुचेरी (2,739 दिन – 7 वर्ष से अधिक): यह केंद्र शासित प्रदेश सरकारी अस्थिरता और दलबदल की राजनीति के कारण बार-बार राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत आया।
- उत्तर प्रदेश और मणिपुर में भी 10 बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका हैं।
राष्ट्रपति शासन: आलोचना और सुधार के सुझाव
- राष्ट्रपति शासन की आलोचना
- केंद्र सरकार अक्सर राजनीतिक विरोधियों को सत्ता से हटाने के लिए अनुच्छेद 356 का उपयोग करती रही है। उदाहरण: 1977 और 1980 में केंद्र में सरकार बदलने के बाद, 9-9 राज्यों की सरकारों को बर्खास्त कर दिया गया।
- यह संघीय ढांचे (federal structure) को कमजोर करता है क्योंकि राज्यों की स्वायत्तता (autonomy) खत्म हो जाती है। निर्वाचित सरकारों को हटाकर केंद्र सरकार का सीधा नियंत्रण स्थापित किया जाता है, जिससे लोकतांत्रिक संतुलन बिगड़ता है।
- जनता द्वारा चुनी गई राज्य सरकारों को हटाने से लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन होता है। नागरिक कार्यात्मक राज्य सरकार से वंचित हो जाते हैं, और प्रशासन केवल नौकरशाहों के हाथ में चला जाता है।
- कई बार राजनीतिक अस्थिरता, दल-बदल या आंतरिक कलह को आधार बनाकर सरकारों को हटाया गया है, जबकि यह पर्याप्त संवैधानिक आधार नहीं है। उदाहरण के लिए, एस.आर. बोम्मई केस (1994) में कर्नाटक सरकार को बिना बहुमत परीक्षण के ही हटा दिया गया था।
- कोई भी सरकारी कार्य जो धर्मनिरपेक्षता को प्रभावित करता है, उसे अनुच्छेद 356 लगाने का कारण नहीं बनाया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया है कि धर्मनिरपेक्षता की रक्षा के नाम पर अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिए।
- सुधार के लिए सुझाव
- सरकारिया आयोग (1983) की सिफारिशें: अनुच्छेद 356 को अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में ही लागू किया जाना चाहिए। पहले राज्य सरकार को चेतावनी दी जाए, और उसे जवाब देने का पर्याप्त अवसर दिया जाए। राज्य विधानसभा में बहुमत परीक्षण के बिना सरकार को बर्खास्त न किया जाए।
- पुंछी आयोग (2007) की सिफारिशें: पूरे राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने के बजाय, सिर्फ प्रभावित क्षेत्रों में केंद्रीय शासन लगाया जाए। अनुच्छेद 356 को लागू करने से पहले संवैधानिक उपायों को प्राथमिकता दी जाए।
- एस.आर. बोम्मई केस (1994) के दिशा-निर्देश: बहुमत परीक्षण सदन में ही होना चाहिए, राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर सरकार को नहीं हटाया जा सकता। संसद द्वारा मंजूरी मिलने तक राष्ट्रपति विधानसभा को भंग नहीं कर सकते। अदालतें राष्ट्रपति शासन की न्यायिक समीक्षा कर सकती हैं।
|
UPSC पिछले वर्षों के प्रश्न (PYQs) प्रश्न (2017): किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा के निम्नलिखित में से कौन-से परिणामों का होना आवश्यक नहीं है? 1. राज्य विधान सभा का विघटन 2. राज्य के मंत्रिपरिषद का हटाया जाना 3. स्थानीय निकायों का विघटन नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए:
उत्तर: केवल 1 और 3 प्रश्न (2018): यदि भारत का राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन यथा उपबंधित अपनी शक्तियों का किसी विशेष राज्य के संबंध में प्रयोग करता है, तो
उत्तर: 2, उस राज्य के विधानमंडल की शक्तियाँ संसद द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन प्रयोज्य होंगी। |
Explore our Books: https://apnipathshala.com/product-category/books/
Explore Our test Series: https://tests.apnipathshala.com/