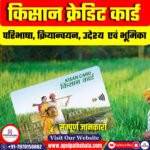|
सामान्य अध्ययन पेपर II: भारतीय संविधान, सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप, राज्य नीति के नीति-निर्देशक सिद्धांत |
चर्चा में क्यों?
पश्चिम बंगाल का नाम बदलने का प्रस्ताव: हाल ही में संसद में तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) ने पश्चिम बंगाल का नाम बदलकर ‘बांग्ला’ करने की मांग उठाई। उनके अनुसार ‘बांग्ला’ नाम राज्य की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत को बेहतर तरीके से प्रदर्शित करता है।
पश्चिम बंगाल का नाम बदलने का प्रस्ताव की पृष्ठभूमि
पश्चिम बंगाल का नाम बदलने की मांग का मुद्दा एक लंबे ऐतिहासिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक संदर्भ में जड़ा हुआ है। यह मांग समय-समय पर सरकारों द्वारा उठाई गई है, लेकिन इसे लेकर अब तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया जा सका है।
- ऐतिहासिक संदर्भ
- 1947 का विभाजन और नामकरण: स्वतंत्रता के बाद, भारत के ब्रिटिश प्रांतों में पंजाब और बंगाल का विभाजन हुआ। पंजाब को “पूर्वी पंजाब” और “पश्चिमी पंजाब” में बांटा गया। लेकिन 1950 में पूर्वी पंजाब का नाम बदलकर केवल “पंजाब” कर दिया गया। बंगाल के मामले में, इसे विभाजित कर “पश्चिम बंगाल” और “पूर्वी पाकिस्तान” (अब बांग्लादेश) नाम दिया गया।
हालांकि, उस समय पश्चिम बंगाल का नाम बदलने की कोई आवश्यकता नहीं समझी गई, क्योंकि प्राथमिकता विभाजन के बाद शरणार्थियों के पुनर्वास, बाढ़ नियंत्रण और औद्योगिक विकास जैसे मुद्दों पर केंद्रित थी। - 1905 का विभाजन: बंगाल पहले भी 1905 में विभाजित हुआ था, जब वायसराय लॉर्ड कर्जन ने “पूर्वी बंगाल और असम” राज्य का गठन किया। उस समय भी राज्य ने अपना नाम “बंगाल” बनाए रखा। 1911 में राष्ट्रवादी आंदोलन के दबाव में विभाजन रद्द कर दिया गया।
- 1947 का विभाजन और नामकरण: स्वतंत्रता के बाद, भारत के ब्रिटिश प्रांतों में पंजाब और बंगाल का विभाजन हुआ। पंजाब को “पूर्वी पंजाब” और “पश्चिमी पंजाब” में बांटा गया। लेकिन 1950 में पूर्वी पंजाब का नाम बदलकर केवल “पंजाब” कर दिया गया। बंगाल के मामले में, इसे विभाजित कर “पश्चिम बंगाल” और “पूर्वी पाकिस्तान” (अब बांग्लादेश) नाम दिया गया।
- सांस्कृतिक संदर्भ
- बंगाल की ऐतिहासिक धरोहर: पश्चिम बंगाल का नाम बदलने की चर्चा केवल प्रशासनिक पहल नहीं है, बल्कि यह बंगाल की सांस्कृतिक पहचान, इतिहास और विरासत से गहराई से जुड़ी हुई है। “बंगाल” शब्द प्राचीन वंग राज्य से जुड़ा है, जिसका उल्लेख महाभारत, पुराणों और गुप्त साम्राज्य के अभिलेखों में मिलता है। यह क्षेत्र न केवल भारतीय इतिहास में बल्कि विश्व इतिहास में अपनी साहित्यिक, बौद्धिक और क्रांतिकारी परंपरा के लिए जाना जाता है।
- सांस्कृतिक पुनर्जागरण: बंगाल 19वीं सदी के सांस्कृतिक पुनर्जागरण और भाषाई आंदोलन का केंद्र था। इस क्षेत्र ने भारत को रवींद्रनाथ ठाकुर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, और काजी नजरुल इस्लाम जैसे महान साहित्यकार दिए, जिनकी कृतियाँ बंगाली भाषा और संस्कृति की पहचान हैं। नाम बदलने की मांग “बांग्ला” भाषा और उसकी विरासत को और अधिक प्रमुखता देने के प्रयास का एक हिस्सा है।
- नाम बदलने की मांग का उद्गम
- 1999 में ज्योति बसु सरकार का प्रस्ताव: पश्चिम बंगाल का नाम बदलने का पहला आधिकारिक प्रस्ताव 1999 में वाम मोर्चा सरकार द्वारा रखा गया। उन्होंने राज्य का नाम “पश्चिम बांग्ला” या “बांग्ला” रखने का सुझाव दिया। हालांकि, यह प्रस्ताव केंद्र सरकार द्वारा कभी स्वीकार नहीं किया गया।
- ममता बनर्जी की पहल (2011 और 2018): 2011 में तृणमूल कांग्रेस की सरकार ने नाम बदलने का मुद्दा दोबारा उठाया। ममता बनर्जी ने तर्क दिया कि “W” से शुरू होने के कारण राज्य को केंद्र की बैठकों में अक्सर चर्चा के लिए अंतिम में बुलाया जाता है, जिससे उसका प्रभाव कम होता है। वर्ष 2016 में भी इसका प्रस्ताव केंद्र को भेजा गया लेकिन उसे भी निरस्त कर दिया गया।
2018 में, विधानसभा ने सर्वसम्मति से “बांग्ला” नाम का प्रस्ताव पारित किया। बंगाली में इसे “बांग्ला”, हिंदी में “बंगाल” और अंग्रेज़ी में “Bengal” कहा जाना प्रस्तावित था। - राजनीतिक और प्रशासनिक विरोध: वर्तमान केंद्रीय सरकार ने इसका विरोध करते हुए “बांग्ला बचाओ हस्ताक्षर अभियान” चलाया। इसके बाद केंद्र ने 2018 के प्रस्ताव को खारिज कर दिया, और राज्य से केवल एक नाम सुझाने को कहा। तब से अब तक यह प्रस्ताव मंजूरी मिलने के लिए केंद्र सरकार के पास अटका हुआ हैं। केंद्र सरकार के अनुसार “बंगाल” का बांग्लादेश के साथ समान नाम होने से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भ्रम की स्थिति पैदा हो सकती है।
संविधान के तहत राज्य का नाम बदलने की प्रक्रिया
भारत में किसी राज्य का नाम बदलने की प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 3 और 4 के तहत तय की गई है। यह प्रक्रिया कानूनी और संवैधानिक रूप से एक सुव्यवस्थित ढांचे के तहत पूरी की जाती है।
- नाम बदलने की प्रक्रिया की शुरुआत: राज्य का नाम बदलने की प्रक्रिया की शुरुआत संसद या राज्य विधानमंडल दोनों में से किसी के माध्यम से हो सकती है। इसमें राज्य स्वयं नाम बदलने का प्रस्ताव भेजता है या केंद्र सरकार भी राज्य का नाम बदलने की प्रक्रिया शुरू कर सकती है।
- यदि राज्य सरकार नाम बदलने का प्रस्ताव भेजती है, तो गृह मंत्रालय उस प्रस्ताव का अध्ययन करता है।
- इसके बाद, प्रस्ताव को केंद्रीय मंत्रिमंडल (Union Cabinet) के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है।
- केंद्रीय मंत्रिमंडल की स्वीकृति के बाद, संविधान संशोधन विधेयक संसद में पेश किया जाता है।
- अनुच्छेद 3 के तहत प्रक्रिया: संसद में राज्य का नाम बदलने के लिए विधेयक (Bill) पेश किया जाता है। विधेयक को पेश करने से पहले, राष्ट्रपति की सिफारिश की आवश्यकता होती है। राष्ट्रपति इस विधेयक को संबंधित राज्य विधानसभा के पास उनकी राय जानने के लिए भेजते हैं।
- राज्य विधानसभा की राय: राज्य विधानसभा को निर्धारित समय के भीतर विधेयक पर अपनी राय व्यक्त करनी होती है। राज्य विधानसभा की राय केवल सुझाव के रूप में मानी जाती है। यह न तो राष्ट्रपति पर बाध्यकारी है और न ही संसद पर।
- विधेयक का संसद में परिचय: निर्धारित समय सीमा समाप्त होने के बाद, विधेयक को संसद में पेश किया जाता है। विधेयक को सरल बहुमत (Simple Majority) से संसद के दोनों सदनों (लोकसभा और राज्यसभा) में पारित करना होता है।
- राष्ट्रपति की मंजूरी: संसद से पारित होने के बाद, विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा जाता है। राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद, विधेयक कानून बन जाता है और राज्य का नाम औपचारिक रूप से बदल दिया जाता है।
- संविधान की अनुसूची-1 में संशोधन: किसी भी राज्य का नाम बदलने के लिए, संविधान की अनुसूची-1 (Schedule-1) में संशोधन किया जाता है। यह संशोधन उस राज्य के नए नाम को आधिकारिक रूप से शामिल करता है।
पश्चिम बंगाल का नाम बदलने का प्रस्ताव के आर्थिक और राजनीतिक प्रभाव
- आर्थिक प्रभाव: नाम बदलने के साथ सभी सरकारी दस्तावेज़, कार्यालय साइनबोर्ड, मानचित्र, स्टेशनरी, पासपोर्ट, और लाइसेंस में बदलाव करना होगा। यह एक लंबी और महंगी प्रक्रिया साबित होती है। इससे निजी संस्थानों को भी अपने दस्तावेज़, बोर्ड, और विज्ञापन सामग्रियों में बदलाव करना होगा, जिससे उनका अतिरिक्त व्यय बढ़ेगा। परिवहन, रेलवे, और हवाई अड्डों के साइनबोर्ड बदलने में भी लाखों रुपये खर्च हो सकते हैं। नाम बदलने की प्रक्रिया में ध्यान और संसाधनों का उपयोग होने से विकास परियोजनाओं पर ध्यान कम हो सकता है।
- सभी सरकारी और कानूनी दस्तावेजों को नए नाम के अनुसार अद्यतन करना एक व्यापक और समय लेने वाली प्रक्रिया है। सभी डिजिटल और मैनुअल रिकॉर्ड में बदलाव करने से प्रशासन पर अतिरिक्त दबाव पड़ सकता है।
- राजनीतिक प्रभाव: नाम बदलना एक समुदाय के लिए अपनी संस्कृति और पहचान को पुनर्स्थापित करने का अवसर हो सकता है। यह कदम अक्सर राजनीतिक दलों के वोट बैंक को मजबूत करने का साधन बन जाता है। नाम बदलना कई बार इतिहास को एक विशेष दृष्टिकोण से प्रस्तुत करने का प्रयास होता है, जो विवाद का कारण बन सकता है। इससे विभिन्न समुदायों के बीच असंतोष बढ़ सकता है, जो सामाजिक तनाव को जन्म दे सकता है।
आजादी के बाद राज्य के नाम बदलने के उदाहरण
भारत में स्वतंत्रता के बाद कई राज्यों ने अपने नाम बदले हैं, और यह नाम बदलने की प्रक्रिया समाजिक, सांस्कृतिक, और राजनीतिक कारणों से जुड़ी हुई है।
- आंध्र प्रदेश: आंध्र प्रदेश का नाम आंध्र राज्य से बदलकर 1 नवंबर 1956 को आंध्र प्रदेश किया गया था। इससे पहले 1953 में मद्रास प्रेसीडेंसी के तेलुगू भाषी हिस्से को आंध्र राज्य का दर्जा दिया गया था। आंध्र प्रदेश का नाम बदलने का उद्देश्य राज्य के लोगों की संस्कृति और पहचान को स्थापित करना था, जो तेलुगू भाषा और उसकी सांस्कृतिक धरोहर को सम्मानित करता था।
- केरल: 1 नवंबर 1956 को त्रावणकोर-कोचीन का नाम बदलकर केरल किया गया था। इस नाम परिवर्तन का उद्देश्य राज्य की संस्कृति, भाषा, और पहचान को एकजुट करना था। केरल शब्द ने यहाँ के लोगों की एकता और विविधता को सम्मिलित किया, जो मलयालम भाषा और हिंदू धर्म की गहरी जड़ों को दर्शाता है।
- मध्य प्रदेश: 1959 में मध्य भारत का नाम बदलकर मध्य प्रदेश कर दिया गया था। यह बदलाव भौगोलिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण था, क्योंकि मध्य भारत की स्थिति भारत के केंद्र में थी, और इसका नामकरण प्रदेश की राजनीतिक और सामाजिक भिन्नताओं को एकजुट करने की दिशा में कदम था। ।l
- तमिलनाडु: मद्रास स्टेट का नाम बदलकर 14 जनवरी 1969 को तमिलनाडु रखा गया। इस नाम बदलने के पीछे प्रमुख कारण था तमिल भाषा और संस्कृति का सम्मान और उसे उभारना। तमिलनाडु का नामकरण तमिलनाडु आंदोलन और सांस्कृतिक अस्मिता के पुनर्निर्माण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम था।
- उत्तर प्रदेश: उत्तर प्रदेश का नाम पहले यूनाइटेड प्रोविंस था, जिसे 24 जनवरी 1950 को बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया। यह बदलाव राज्य की सांस्कृतिक और राजनीतिक पहचान को पुनर्परिभाषित करने का हिस्सा था।
- उत्तराखंड: 2007 में उत्तरांचल का नाम बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया। उत्तरांचल का नाम बदलने का मुख्य कारण था उत्तर प्रदेश से अलग होने के बाद हिमालयी राज्य की पहचान को मजबूत करना। उत्तराखंड नाम का चयन राज्य के प्राकृतिक सौंदर्य, सांस्कृतिक विविधता, और हिमालय पर्वतों से जुड़ी विशिष्टता को दर्शाने के लिए किया गया।
- उड़ीसा से ओडिशा: नवंबर 2011 में उड़ीसा का नाम बदलकर ओडिशा किया गया था। यह नाम परिवर्तन ओडिया भाषा के सम्मान में था, क्योंकि उड़ीसा शब्द की उत्पत्ति हिंदी से हुई थी, जबकि राज्य की मुख्य भाषा ओडिया है।
- पुडुचेरी: पॉन्डिचेरी का नाम 1 अक्टूबर 2006 को पुडुचेरी रखा गया। इस नाम परिवर्तन का उद्देश्य फ्रांसीसी उपनिवेश की पहचान को समाप्त करना था, और यह राज्य के इतिहास और पहचान को भारतीय संदर्भ में लाने का प्रयास था।
- केरल : केरल सरकार ने राज्य का नाम बदलकर केरलम करने का प्रस्ताव दिया है, जो मलयालम में ही अधिक उपयुक्त और लोकप्रिय है। अभी तक केंद्र से इसे मंजूरी नहीं मिली है।
|
UPSC पिछले वर्षों के प्रश्न (PYQs) प्रश्न (2021): 26 जनवरी, 1950 को भारत की वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या थी? (a) एक लोकतांत्रिक गणराज्य (b) एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य (c) एक संप्रभु धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य (d) एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य उत्तर: (b) प्रश्न (2012): भारतीय संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण निम्नलिखित में दी गई योजना पर आधारित है: (a) मॉर्ले-मिंटो सुधार, 1909 (b) मोंटेग्यू-चेम्सफोर्ड अधिनियम, 1919 (c) भारत सरकार अधिनियम, 1935 (d) भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947 उत्तर: (c) |
Explore our Books: https://apnipathshala.com/product-category/books/
Explore Our test Series: https://tests.apnipathshala.com/