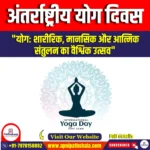Download Today Current Affairs PDF
संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष (UNFPA) ने भारत की मातृ स्वास्थ्य और परिवार नियोजन में उल्लेखनीय प्रगति की सराहना की है। UNFPA की कार्यकारी निदेशक डॉ. नतालिया कनम ने केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव श्रीमती पुण्य सलिला श्रीवास्तव को इस प्रगति के लिए पट्टिका और प्रमाण पत्र प्रदान किया, जो भारत द्वारा महिलाओं के स्वास्थ्य और कल्याण में किए गए सुधारों का प्रतीक है।
भारत में मातृ स्वास्थ्य और परिवार नियोजन को सुधारने के लिए मुख्य पहलें:
भारत में मातृ स्वास्थ्य और परिवार नियोजन को सुधारने के लिए कई महत्वपूर्ण पहल की गई हैं, जिनका उद्देश्य माताओं और नवजात शिशुओं के स्वास्थ्य को बेहतर बनाना है। इन पहलों के माध्यम से भारत ने मातृ और शिशु स्वास्थ्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है।
- सुरक्षित मातृत्व आश्वासन योजना (सुमन):
- बिना किसी लागत के गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं को गुणवत्तापूर्ण, गरिमापूर्ण और सम्मानजनक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना।
- सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं में किसी भी महिला या नवजात शिशु को सेवाओं से इनकार करने के प्रति शून्य सहिष्णुता की नीति।
- प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान (PMSMA):
- सभी गर्भवती महिलाओं को नि:शुल्क और व्यापक प्रसवपूर्व देखभाल प्रदान करना।
- इस अभियान के तहत गर्भवती महिलाओं की नियमित जांच और देखभाल सुनिश्चित की जाती है, जिससे प्रसव के दौरान जटिलताओं को कम किया जा सके।
- मिडवाइफरी सेवा पहल:
- इस पहल के अंतर्गत लगभग 90,000 दाइयों को प्रशिक्षण दिया जाएगा।
- प्रशिक्षित दाइयां यौन, प्रजनन, मातृ, नवजात और किशोर स्वास्थ्य (SRMNAH) देखभाल का 90% प्रदान करने में सक्षम होंगी, जिससे ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित हो सके।
मातृ स्वास्थ्य और परिवार नियोजन में भारत की प्रगति:
- मातृ मृत्यु दर (MMR):
- भारत ने 2000 और 2020 के बीच मातृ मृत्यु दर को 70% घटाकर 97 (प्रति 1,00,000 जीवित जन्म) कर दिया है।
- भारत 2030 तक MMR को 70 से कम करने के एसडीजी लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है।
- कुल प्रजनन दर (TFR): 2020 में कुल प्रजनन दर 2.0 हो गई, जो प्रतिस्थापन स्तर प्रजनन दर (2.1) से कम है, जो परिवार नियोजन की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।
- संस्थागत प्रसव:
- 2019-2021 में 89% महिलाओं ने स्वास्थ्य सुविधाओं में प्रसव कराया, जो 2015-2016 में 79% था।
- यह संस्थागत प्रसव में वृद्धि स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच और गुणवत्ता में सुधार को दर्शाती है।
- शिशु मृत्यु दर (IMR):
- 2014 में शिशु मृत्यु दर 39 थी, जो 2020 में घटकर 28 हो गई है।
- यह शिशु स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार का संकेत है, जिससे नवजात शिशुओं की मृत्यु दर में कमी आई है।
संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष (UNFPA) के बारे में :
UNFPA (संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष) संयुक्त राष्ट्र की एक महत्वपूर्ण एजेंसी है, जिसका उद्देश्य यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य और अधिकारों को सुनिश्चित करना है। इसकी स्थापना 1967 में एक ट्रस्ट फंड के रूप में हुई थी और 1969 में इसे जनसंख्या गतिविधियों के लिए संयुक्त राष्ट्र कोष के रूप में मान्यता मिली। 1987 में इसका नाम बदलकर संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष (UNFPA) कर दिया गया।
UNFPA के मुख्य उद्देश्य:
- हर गर्भावस्था वांछित हो – यह सुनिश्चित करना कि प्रत्येक महिला को अपनी गर्भावस्था की योजना और देखभाल का अधिकार हो।
- हर प्रसव सुरक्षित हो – प्रसव के दौरान महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना।
- हर युवा की क्षमता पूरी हो – युवाओं को उनकी पूरी क्षमता तक पहुँचने में मदद करना।
आदर्श वाक्य:
“सभी के लिए अधिकार और विकल्प सुनिश्चित करना।”
UNFPA की भूमिका:
- यह एजेंसी संयुक्त राष्ट्र महासभा और आर्थिक एवं सामाजिक परिषद (ECOSOC) से समग्र नीतिगत मार्गदर्शन प्राप्त करती है।
- यह दुनिया भर में 150 से अधिक देशों में यौन और प्रजनन स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच बढ़ाने के लिए काम करता है।
- UNFPA लैंगिक समानता को बढ़ावा देता है और महिलाओं, लड़कियों और युवाओं को सशक्त बनाता है ताकि वे अपने शरीर और भविष्य पर नियंत्रण रख सकें।
मुख्य लक्ष्य:
- 2030 तक परिवार नियोजन की अपूर्ण आवश्यकताओं को पूरा करना।
- रोके जा सकने वाली मातृ मृत्यु, लिंग आधारित हिंसा, बाल विवाह और महिला जननांग विकृति जैसी हानिकारक प्रथाओं को समाप्त करना।
UNFPA वैश्विक स्तर पर महिलाओं और युवाओं के स्वास्थ्य और अधिकारों की रक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण एजेंसी है, जो लैंगिक समानता को बढ़ावा देने और सशक्तिकरण की दिशा में कार्यरत है।
Explore our Books: https://apnipathshala.com/product-category/books/
Explore Our test Series: https://tests.apnipathshala.com/